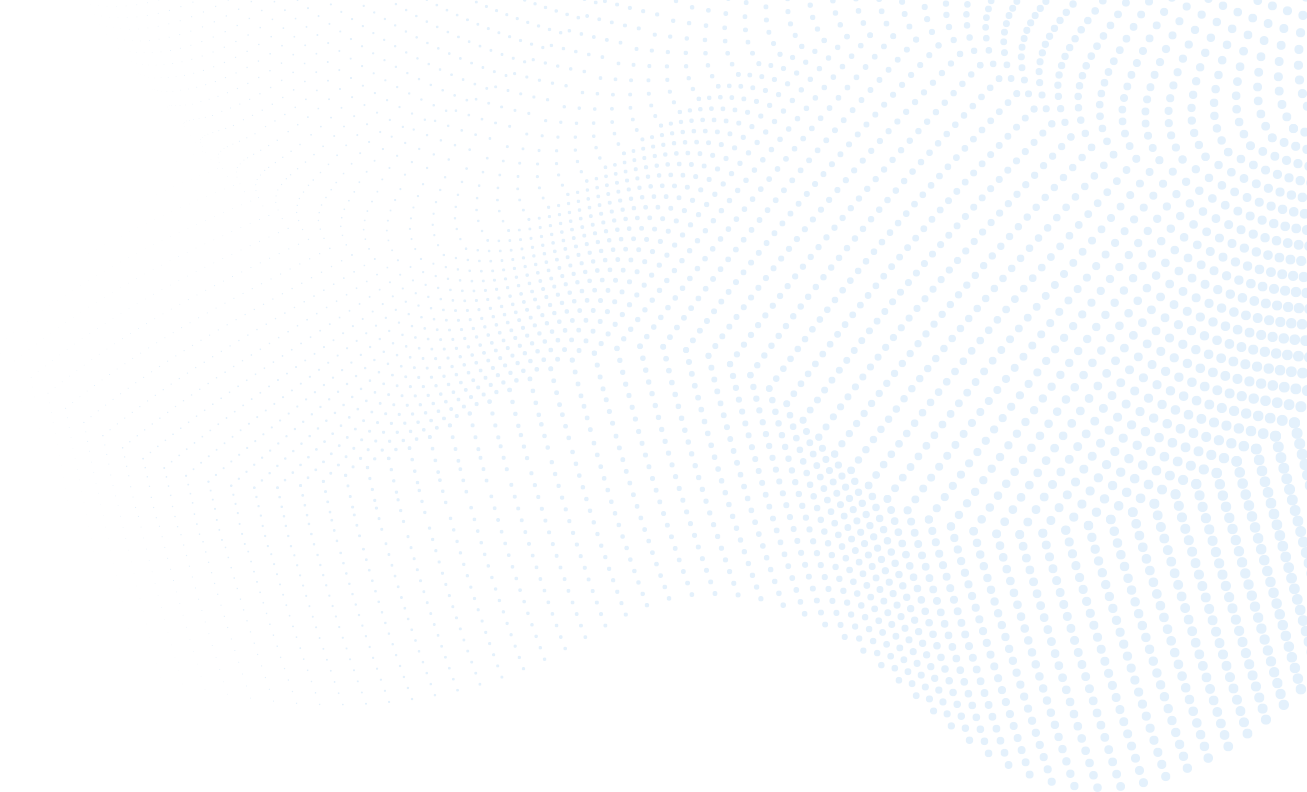
उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया?
हम यहां इस्लाम के प्रति एक ईमानदार, शांत और सम्मानजनक दृष्टिकोण खोलने के लिए आये हैं।
इस पृष्ठ पर, हम विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों की कहानियों को उजागर कर रहे हैं, जिन्होंने शोध और चिंतन के बाद दृढ़ विश्वास के साथ इस्लाम को चुना।
ये केवल व्यक्तिगत कहानियां नहीं हैं, बल्कि ईमानदार गवाहियां हैं जो इस्लाम द्वारा उनके दिलों और दिमागों में लाए गए गहन परिवर्तन, उनके प्रश्नों के उत्तर तथा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनके द्वारा महसूस किए गए आश्वासन को व्यक्त करती हैं।
चाहे कहानी दार्शनिक जांच से शुरू हुई हो, जिज्ञासा से प्रेरित हो, या यहां तक कि एक मार्मिक मानवीय रुख से, इन अनुभवों में आम बात यह है कि उन्हें इस्लाम में प्रकाश मिला, और संदेह के स्थान पर निश्चितता आई।
हम इन कहानियों को विभिन्न भाषाओं में, लिखित और दृश्य प्रारूपों में प्रस्तुत करते हैं, ताकि ये प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करें और जीवंत मानवीय अनुभव के माध्यम से इस्लाम का सच्चा परिचय दें।

महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया
सलमान अल-फ़ारसी - सत्य का खोजी

यह एक कहानी थी. महान साथी सलमान अल-फ़ारसी प्रेरणा के स्रोत और सत्य की खोज में धैर्य और दृढ़ता के एक सच्चे उदाहरण, सलमान (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) इस्लाम के आगमन से पहले पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म के बीच रहे। उन्होंने सच्चे धर्म की खोज तब तक जारी रखी जब तक अल्लाह ने उन्हें उस तक पहुँचाया। उन्होंने अपने मन और हृदय को अपनी मातृभूमि की परंपराओं और विरासत में मिली मान्यताओं के अधीन नहीं किया, यदि वे अपनी मृत्यु तक इन परंपराओं का पालन करते, तो वे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथियों में शामिल नहीं होते। उन्हें इस्लाम धर्म का मार्गदर्शन नहीं मिलता और वे एक बहुदेववादी के रूप में मरते।
हालाँकि सलमान फारसी अग्नि पूजा के बीच फारस में पले-बढ़े थे, फिर भी वे सच्चे धर्म की खोज में ईश्वर की खोज में निकल पड़े। वे पारसी थे, लेकिन इस धर्म से सहमत नहीं थे। हालाँकि, उन्होंने पाया कि उनके पूर्वज भी इस धर्म के प्रति समर्पित थे, इसलिए उन्होंने भी इसे अपना लिया। जब अपने और अपने परिवार के धर्म के बारे में उनके मन में संदेह गहरा गया, तो सलमान अपना देश, फारस छोड़कर, परम धार्मिक सत्य की खोज में लेवंत चले गए। वहाँ उनकी मुलाक़ात भिक्षुओं और पुजारियों से हुई। एक लंबी यात्रा के बाद, सलमान एक गुलाम के रूप में मदीना पहुँचे। जब उन्होंने पैगंबर ﷺ के बारे में सुना, तो उनसे मिले और उनके संदेश से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया।
उस महान साथी ने बताया कि वह इस्फ़हान (वर्तमान ईरान) की धरती पर एक फ़ारसी के रूप में पैदा हुआ था। वह जी नामक एक गाँव के लोगों के यहाँ पैदा हुआ था और उसके पिता उसके शासक थे। सलमान एक कुलीन परिवार में पले-बढ़े थे और फ़ारस में हमेशा सुख-सुविधाओं से जीवन व्यतीत करते थे। उनके पिता उनसे बेहद प्यार करते थे और उनके लिए इतना डरते थे कि उन्होंने उन्हें अपने घर में कैद कर लिया था। सलमान ने पारसी धर्म में तब तक प्रगति की जब तक कि वह अग्नि के वासी नहीं बन गए, उसे जलाते और एक घंटे तक उसे बुझने नहीं देते थे।
एक दिन, उसके पिता ने उसे अपने खेत की देखभाल करने के लिए बुलाया क्योंकि वह व्यस्त था। उन्होंने उससे कहा कि वह देर न करे ताकि उसे चिंता न हो। खेत जाते हुए, सलमान एक चर्च के पास से गुज़रा जहाँ लोग प्रार्थना कर रहे थे। वह अंदर गया और उनसे प्रभावित हुआ। उसने कहा, "अल्लाह की कसम, यह हमारे धर्म से बेहतर है।" वह सूरज ढलने तक वहाँ से नहीं गया।
उसने उनसे इस धर्म की उत्पत्ति के बारे में पूछा, और उन्होंने बताया कि यह लेवेंट में है। तब सलमान अपने पिता के पास लौटा और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, और यह भी कि वह इस धर्म से इतना प्रभावित हुआ था कि उसे लगा कि वह ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है।
सलमान ने बताया, "मैंने ईसाइयों के पास संदेश भेजा और कहा: 'अगर सीरिया से ईसाई व्यापारियों का एक समूह तुम्हारे पास आए, तो मुझे उनके बारे में सूचित करो।' इसलिए सीरिया से ईसाई व्यापारियों का एक समूह उनके पास आया और उन्होंने उसे सूचित किया। वह अपने पिता के घर से भागकर सीरिया चला गया।"
वहाँ उसकी मुलाक़ात एक तपस्वी बिशप से हुई जो सही रास्ते पर था, और जब मौत उसके क़रीब आई, तो उसने उसे मोसुल के एक बिशप के पास जाने की सलाह दी जो अभी भी धर्मनिष्ठ था और पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मिशन का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए वह उसके पास गया और कुछ समय तक उसके साथ रहा, फिर मौत उसके क़रीब आई और उसने उसे निसिबिस के एक बिशप के पास जाने की सलाह दी। यही बात फिर दोहराई गई, जब तक कि वह रोम के अमोरियम के एक बिशप के पास नहीं पहुँचा, जिसने उसे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के समय के बारे में बताया। बिशप ने उससे कहा: "मेरे बेटे, अल्लाह की कसम, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो हमारे जैसा बचा हो। मैं तुम्हें उसके पास जाने का आदेश देता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक नबी का समय आ गया है। उसे पवित्र स्थान से भेजा जाएगा, जो दो लावा क्षेत्रों के बीच से होकर ताड़ के पेड़ों वाली एक नमकीन भूमि पर जाएगा। उसके पास ऐसी निशानियाँ होंगी जिन्हें छिपाया नहीं जा सकेगा। उसके कंधों के बीच नबी होने की मुहर होगी। वह उपहार खाएगा, लेकिन दान नहीं। अगर तुम उस देश तक पहुँच सको, तो पहुँच जाओ, क्योंकि उसका समय तुम्हारे ऊपर आ गया है।"
फिर अरबों की भूमि से एक कारवां सलमान के पास से गुजरा, इसलिए वह अंत समय के पैगंबर की तलाश में उनके साथ चला गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने उसे एक यहूदी को बेच दिया और वह मदीना पहुंचा और वहां के खजूर के पेड़ों से पहचान गया कि यह पैगंबर का शहर था, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, जैसा कि बिशप ने उसे बताया था।
सलमान पैगंबर के मदीना आगमन की कहानी सुनाते हुए कहते हैं: "अल्लाह ने अपने पैगंबर, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, को मक्का भेजा, और मैंने गुलामी के बावजूद उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, जब तक कि अल्लाह के रसूल, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, कुबा नहीं पहुँचे, और मैं अपने साथी के लिए उनके ताड़ के बाग में काम कर रहा था। जब मैंने पैगंबर के आगमन की खबर सुनी, तो मैं नीचे गया और पूछा: 'यह क्या खबर है?' मेरे मालिक ने अपना हाथ उठाया और मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा, और कहा: 'इससे तुम्हारा क्या लेना-देना है? जाओ अपना काम करो।'"
सलमान पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उन खूबियों को परखना चाहता था जिनके बारे में बिशप ने उसे बताया था, यानी कि वह दान नहीं करते थे, दान स्वीकार करते थे, और उनके कंधों के बीच नबूवत की मुहर होती थी, और भी कई निशानियाँ। इसलिए वह शाम को पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास गया, अपने साथ कुछ खाना ले गया और उनसे कहा कि यह खाना दान का है। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने साथियों को खाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। सलमान समझ गया कि यह भी उन्हीं निशानियों में से एक थी।
फिर वह फिर से पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास लौटा और उनके लिए खाना इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यह एक उपहार है। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे खाया और उनके साथियों ने भी खाया, इसलिए उन्हें पता चला कि यह दूसरी निशानी है।
सलमान ने नबूवत की मुहर की खोज की और वह इसके बारे में कहते हैं: "फिर मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया, जब वह एक जनाज़े के जुलूस के पीछे चल रहे थे। मैंने अपने दो लबादे पहने हुए थे और वह अपने साथियों के साथ थे। मैं उनकी पीठ की ओर देखने के लिए मुड़ा, यह देखने के लिए कि क्या मैं वह मुहर देख सकता हूँ जिसका वर्णन मुझे किया गया था। जब उन्होंने मुझे अपनी ओर मुड़ते देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसी बात की पुष्टि कर रहा हूँ जिसका वर्णन मुझे किया गया था, इसलिए उन्होंने अपना लबादा उतार फेंका। मैंने मुहर को देखा और उसे पहचान लिया, इसलिए मैं उन पर गिर पड़ा, उसे चूमा और रोया।" इस प्रकार, फ़ारसी सलमान ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपने गुरु को पत्र लिखा। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने साथियों से उनकी मदद करने के लिए कहा। सलमान को रिहा कर दिया गया और वह पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथी बने रहे, उनका अनुसरण करते हुए, यहाँ तक कि पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "सलमान हम में से हैं, पैगंबर के परिवार से।"
सलमान अल-फ़ारसी का सत्य तक पहुँचने का सफ़र लंबा और कठिन था। उन्होंने फ़ारस में पारसी धर्म से, फिर लेवंत में ईसाई धर्म अपनाया, फिर अरब प्रायद्वीप में गुलामी की ओर रुख़ किया, जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और इस्लाम की ओर निर्देशित नहीं किया।
उमर इब्न अल-खत्ताब (मुसलमानों के सबसे शत्रुतापूर्ण लोगों में से एक, लेकिन मुसलमानों का खलीफा)
 उमर इब्न अल-खत्ताब, रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथी, बलवान और प्रभावशाली थे। उन्होंने छब्बीस साल की उम्र में इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों में उनका स्थान उनतीसवें स्थान पर था, यानी इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों में उनका स्थान चालीसवाँ था और उनकी उम्र पचास या छप्पन बताई गई थी।
उमर इब्न अल-खत्ताब, रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथी, बलवान और प्रभावशाली थे। उन्होंने छब्बीस साल की उम्र में इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों में उनका स्थान उनतीसवें स्थान पर था, यानी इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों में उनका स्थान चालीसवाँ था और उनकी उम्र पचास या छप्पन बताई गई थी।
उमर इब्न अल-खत्ताब - ईश्वर उनसे प्रसन्न हों - इस्लाम धर्म अपनाने से पहले मुसलमानों के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण लोगों में से एक थे।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दुआ की और कहा: "हे ईश्वर, इन दो लोगों में से जो आपको सबसे प्रिय हैं, अबू जहल या उमर इब्न अल-खत्ताब, उनके द्वारा इस्लाम को मज़बूत करें।" उन्होंने कहा: "उन्हें सबसे प्रिय व्यक्ति उमर थे।" और वास्तव में, उमर ने इस्लाम में प्रवेश किया।
उमर इब्न अल-खत्ताब के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
साथी उमर इब्न अल-खत्ताब (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के इस्लाम में धर्म परिवर्तन की कहानी का क्रम इस प्रकार है: उमर इब्न अल-खत्ताब ने पैगंबर मुहम्मद को मारने का फैसला किया। कुरैश पैगंबर मुहम्मद को मारना चाहते थे, और उन्होंने उन्हें मारने के मामले और कौन आदमी उन्हें मारेगा, इस बारे में परामर्श किया। उमर ने स्वेच्छा से, इसलिए वह एक बहुत ही गर्म दिन में अपनी तलवार लेकर अल्लाह के रसूल (शांति और आशीर्वाद उन पर हो) के पास गए। रसूल अपने साथियों के साथ बैठे थे, जिनमें अबू बक्र अल-सिद्दीक, अली और हमजा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) शामिल थे, और कुछ साथी जो अल्लाह के रसूल के साथ रहे और हबश नहीं गए। उमर इब्न अल-खत्ताब को पता था कि वे अल-सफा के तल पर अल-अर्कम के घर में इकट्ठे हुए उसने उसे रोका और पूछा: "तुम कहाँ जा रहे हो?" उसने बताया कि वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उनके देवताओं का अपमान किया है और उनके धर्म को तुच्छ जाना है। दोनों व्यक्ति एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे, और उसने उससे कहा, "उमर, तुमने कितना बुरा रास्ता अपनाया है।" उसने उसे बनू अब्द मनाफ की ताकत की याद दिलाई और कहा कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उमर ने उससे पूछा कि क्या उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है ताकि वह उसे मारना शुरू कर सके। जब नुआइम ने देखा कि वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मारने के अपने इरादे को नहीं छोड़ेगा, तो उसने उसे यह कहकर रोका कि उसका परिवार, उसकी बहन, उसका पति और उसका चचेरा भाई, सभी इस्लाम धर्म अपना चुके हैं।
अपनी बहन के इस्लाम धर्म अपनाने पर उमर इब्न अल-खत्ताब का रुख
नुआइम द्वारा अपनी बहन के इस्लाम धर्म अपनाने की सूचना मिलने के बाद, उमर इब्न अल-खत्ताब अपनी बहन के घर शिकायत करने गए। उनकी बहन फ़ातिमा और उनके पति सईद ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और उनके साथी ख़ब्बाब इब्न अल-अरत उन्हें क़ुरान पढ़ा रहे थे। जब उमर पहुँचे, तो ख़ब्बाब फ़ातिमा और उनके पति सईद (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) को क़ुरान सुना रहे थे। यह क़ुरान सूरह ताहा से था। उमर ने उन्हें सुना, और जब वे अंदर गए, तो ख़ब्बाब छिप गए। उमर ने उनसे उस आवाज़ के बारे में पूछा जो उन्होंने सुनी थी, और उन्होंने उन्हें बताया कि यह उनके बीच की बातचीत थी। उमर ने कहा, "शायद तुम दोनों भटक गए हो।" सईद ने उससे कहा, "उमर, मुझे बताओ कि क्या सच्चाई तुम्हारे धर्म के अलावा किसी और में है?" उमर उन्हें मारने के लिए उठे, लेकिन फ़ातिमा ने उन्हें रोक दिया, इसलिए उन्होंने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से जवाब दिया, "ऐ उमर, अगर सच्चाई तुम्हारे धर्म में नहीं है," जब उमर उनसे निराश हो गए, तो उन्होंने वह किताब मांगी जो वे पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बहन ने उन्हें तब तक किताब नहीं दी जब तक कि वह खुद को शुद्ध नहीं कर लेते। उन्होंने उसकी बात मान ली और खुद को शुद्ध किया, फिर किताब ली और सूरत ताहा से पढ़ा जब तक कि वह इस आयत तक नहीं पहुँच गए, "वास्तव में, मैं अल्लाह हूँ। मेरे अलावा कोई पूज्य नहीं है, इसलिए मेरी पूजा करो और मेरी याद के लिए नमाज़ स्थापित करो।" [ताहा: 14] उमर अपने द्वारा पढ़े गए शब्दों की सुंदरता पर चकित थे। उस समय, खब्बाब बाहर आए और उन्हें बताया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, ने उनके इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना की थी।
उमर इब्न अल-खत्ताब द्वारा पैगंबर की उपस्थिति में इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा
जब उमर ने आयतें पढ़ीं, तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने खब्बाब से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ठिकाने के बारे में पूछा ताकि वह उनके पास जाकर उनके इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा कर सके। खब्बाब ने बताया कि वह अरक़म इब्न अबी अरक़म के घर में हैं। उमर ने जाकर अरक़म के घर में मौजूद साथियों का दरवाज़ा खटखटाया। उमर की आवाज़ सुनकर वे चौंक गए और डर गए। हालाँकि, हमज़ा ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, "अगर अल्लाह ने उसके लिए अच्छा चाहा, तो वह मुसलमान हो जाएगा, और अगर वह कुछ और चाहेगा, तो उसे मारना हमारे लिए आसान होगा।" वे उसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास ले गए। हमज़ा और एक अन्य व्यक्ति ने उमर को बाँहों से पकड़ा और उसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास ले गए। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) खड़े हुए और उन्हें उसे अकेला छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों आया है। उमर ने तब उससे कहा कि वह इस्लाम धर्म अपनाना चाहता है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाहु अकबर का ऐलान किया और घर के सभी लोगों को उसके इस्लाम धर्म अपनाने की खबर पता चल गई। वे इस बात से खुश हुए कि हमज़ा और उमर (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के इस्लाम धर्म अपनाने से वे और भी मज़बूत और शक्तिशाली हो गए हैं।
उमर के इस्लाम धर्म अपनाने का इस्लामी आह्वान पर प्रभाव
उमर इब्न अल-खत्ताब के इस्लाम धर्म अपनाने के कई प्रभाव पड़े। उस समय, मुसलमान खुद को गौरवान्वित, शक्तिशाली और निश्चिंत महसूस करते थे। उनमें से कोई भी खुलेआम नमाज़ नहीं पढ़ सकता था और न ही काबा की परिक्रमा कर सकता था। जब उमर ने इस्लाम धर्म अपनाया, तो उनके साथियों ने नमाज़ पढ़ना और काबा की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। उमर ने मुश्रिकों को अपने इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की, और वे इस दुखद समाचार से बहुत निराश हुए। उन्होंने बिना किसी डर या झिझक के अबू जहल को अपने इस्लाम धर्म अपनाने की सूचना दी। इब्न मसऊद ने इसी अर्थ का उल्लेख करते हुए कहा: "उमर के इस्लाम धर्म अपनाने तक हम काबा में नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे।" इस प्रकार, इस्लाम धर्म अपनाने का आह्वान सार्वजनिक हो गया।
डॉ. इंग्रिड मैटसन
 इसका परिचय
इसका परिचय
डॉ. इंग्रिड मैटसन कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड कॉलेज में धर्म की प्रोफ़ेसर हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण कनाडा के ओंटारियो में हुआ और उन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र और ललित कला की पढ़ाई की है।
मैटसन ने कॉलेज के अंतिम वर्ष के दौरान इस्लाम धर्म अपना लिया और 1987 में पाकिस्तान चली गईं, जहाँ उन्होंने एक साल तक शरणार्थियों के साथ काम किया। उन्होंने 1999 में शिकागो विश्वविद्यालय से इस्लामी अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
उनके इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
इंग्रिड का पालन-पोषण ईसाई धर्म में हुआ था, धार्मिक नहीं। इस्लाम में उनकी शुरुआती रुचि कला के प्रति उनके प्रेम से उपजी थी। डॉ. इंग्रिड टोरंटो, मॉन्ट्रियल और शिकागो के प्रमुख संग्रहालयों की अपनी यात्राओं का वर्णन करती हैं, जब तक कि उन्होंने पेरिस के लूवर संग्रहालय का दौरा नहीं किया और मानव इतिहास में चित्रकला की कला से गहराई से प्रभावित नहीं हुईं।
फिर वह मुसलमानों के एक समूह से मिलीं, और उनके बारे में वह कहती हैं: "मैं ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने अपने ईश्वर की मूर्तियाँ या कामुक चित्र नहीं बनाए थे, और जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस्लाम बुतपरस्ती और लोगों की पूजा से बहुत सावधान है, और ईश्वर को जानना उनकी रचनाओं पर विचार करने से बहुत आसान है।"
इसी दृष्टिकोण से, इंग्रिड ने इस्लाम के बारे में सीखने की अपनी यात्रा शुरू की, जो उनके इस्लाम धर्म अपनाने के साथ समाप्त हुई। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और मिशनरी कार्य के क्षेत्र में प्रवेश किया।
उनका योगदान
इंग्रिड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला इस्लामी धार्मिक कार्यक्रम स्थापित किया। 2001 में, उन्हें इस्लामिक सोसाइटी ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 20,000 सदस्य हैं, और 350 मस्जिदें और इस्लामी केंद्र हैं। मैटसन इस संगठन के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं।
फ्रांसीसी सर्जन मौरिस बुकेले
 मौरिस बुकेले कौन है?
मौरिस बुकेले कौन है?
मौरिस बुकेल का जन्म फ्रांसीसी माता-पिता के यहाँ हुआ था और अपने परिवार की तरह ही उनका पालन-पोषण भी ईसाई धर्म में हुआ। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने फ़्रांस विश्वविद्यालय में चिकित्साशास्त्र की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहाँ वे चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने तक शीर्ष छात्रों में से एक थे। वे आगे बढ़ते हुए आधुनिक फ़्रांस के सबसे प्रसिद्ध और कुशल शल्यचिकित्सक बन गए। शल्य चिकित्सा में उनका कौशल एक अद्भुत कहानी थी जिसने उनके जीवन और उनके अस्तित्व को बदल दिया।
मौरिस बुकेले के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
फ्रांस प्राचीन वस्तुओं और विरासत में अपनी रुचि के लिए जाना जाता है। 1981 में जब दिवंगत फ्रांसीसी समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांस्वा मित्तरैंड ने सत्ता संभाली, तो फ्रांस ने 1980 के दशक के अंत में मिस्र से मिस्र के फ़राओ की ममी को पुरातात्विक परीक्षण और उपचार के लिए रखने का अनुरोध किया।
मिस्र के अब तक के सबसे कुख्यात तानाशाह का शव ले जाया गया, और वहां, हवाई अड्डे पर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, उनके मंत्री और देश के वरिष्ठ अधिकारी एक पंक्ति में खड़े होकर, विमान की सीढ़ियों पर झुककर, मिस्र के फिरौन का शाही स्वागत करने लगे, मानो वह अभी भी जीवित हों!!
जब मिस्र के फ़राओ का शाही स्वागत समारोह फ्रांस में संपन्न हुआ, तो तानाशाह की ममी को उसके स्वागत समारोह से कम भव्य जुलूस में नहीं ले जाया गया। इसे फ्रांसीसी पुरातत्व केंद्र के एक विशेष विंग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ फ्रांस के सबसे प्रमुख पुरातत्वविदों, शल्य चिकित्सकों और शरीर रचना विज्ञानियों ने ममी का अध्ययन और उसके रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। मुख्य शल्य चिकित्सक और इस फ़राओनी ममी के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार व्यक्ति प्रोफ़ेसर मौरिस बुकेल थे।
चिकित्सकों की रुचि ममी को पुनर्स्थापित करने में थी, जबकि उनके प्रमुख, मौरिस बुकेले, किसी और चीज़ में बहुत रुचि रखते थे। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस फ़राओ की मृत्यु कैसे हुई थी, और देर रात, उनके विश्लेषण के अंतिम परिणाम जारी किए गए।
फ्रांसीसी सर्जन मौरिस बुकेले
लेकिन कुछ अजीब बात थी जो अभी भी उसे हैरान कर रही थी: यह शरीर - अन्य ममीकृत फैरोनिक शवों के विपरीत - दूसरों की तुलना में अधिक अक्षुण्ण कैसे रहा, जबकि इसे समुद्र से निकाला गया था?
मौरिस बुकेले एक अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जिसे वे समुद्र से एक फ़राओ के शव की बरामदगी और उसके डूबने के तुरंत बाद उसके ममीकरण में एक नई खोज मान रहे थे, तभी किसी ने उनके कान में फुसफुसाया: जल्दबाजी मत करो; मुसलमान इस ममी के डूबने के बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने इस खबर की कड़ी निंदा की और इस पर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि ऐसी खोज केवल आधुनिक विज्ञान के विकास और आधुनिक, अत्यंत सटीक कंप्यूटरों के माध्यम से ही ज्ञात हो सकती है। एक अन्य व्यक्ति ने यह कहकर उनके आश्चर्य को और बढ़ा दिया: उनका कुरान, जिस पर वे विश्वास करते हैं, उनके डूबने और डूबने के बाद उनके शरीर की सुरक्षा के बारे में एक कहानी बताता है।
वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा: ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस ममी की खोज 1898 ई. तक नहीं हुई थी, अर्थात लगभग दो सौ वर्ष पहले, जबकि उनका कुरान चौदह सौ वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है?!
यह कैसे तर्कसंगत हो सकता है, जब सारी मानवता - न केवल मुसलमान - को प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा अपने फ़राओ के शवों को ममी बनाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, केवल कुछ दशक पहले तक?
उस रात, मौरिस बुकेले फिरौन के शरीर को घूरते हुए बैठे रहे, और उनके साथी ने जो कुछ फुसफुसाकर उनसे कहा था, उसके बारे में गहराई से सोचते रहे: कि मुसलमानों का कुरान डूबने के बाद इस शरीर के जीवित रहने की बात कहता है, जबकि ईसाइयों की पवित्र पुस्तक (मैथ्यू और ल्यूक के सुसमाचार) हमारे स्वामी मूसा (उन पर शांति हो) का पीछा करते हुए फिरौन के डूबने की बात कहती है, उसके शरीर के भाग्य का कोई उल्लेख किए बिना।
वह अपने आप से कहने लगा: क्या यह संभव है कि मेरे सामने खड़ा यह ममीकृत व्यक्ति मिस्र का फिरौन है जो मूसा को सता रहा था?
क्या यह संभव है कि उनके मुहम्मद (ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें) को यह बात एक हजार वर्ष से भी पहले पता थी, और मैं अभी इसके बारे में जान रहा हूँ?
मौरिस बुकेल को नींद नहीं आ रही थी, और उन्होंने टोरा लाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने टोरा से निर्गमन की पुस्तक पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा है: "पानी वापस आ गया और रथों और घुड़सवारों को, यानी फिरौन की पूरी सेना को, जो उनके पीछे समुद्र में गई थी, डुबो दिया। उनमें से एक भी नहीं बचा।" मौरिस बुकेल असमंजस में थे।
यहां तक कि टोरा में भी इस शरीर के जीवित रहने तथा फिरौन के शरीर के उपचार और पुनर्स्थापना के बाद भी इसके अक्षुण्ण बने रहने का उल्लेख नहीं किया गया है।
फ्रांस ने ममी को एक आलीशान काँच के ताबूत में मिस्र लौटा दिया, लेकिन मौरिस बुकेले इस फैसले से बेचैन थे और उन्हें मन की शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि मुसलमानों के बीच ममी की सुरक्षा को लेकर फैली खबरों ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपना सामान पैक किया और सऊदी अरब जाने का फैसला किया, जहाँ वे एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें मुस्लिम शरीर रचना विज्ञानियों का एक समूह शामिल होगा।
और फिरौन के डूबने के बाद उसके शरीर के जीवित रहने के बारे में जो कुछ उसने खोजा था, उसके बारे में उसने उनसे पहली बातचीत की। उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके लिए क़ुरआन खोला, और उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये शब्द पढ़ने लगा: {अतः आज हम तुम्हें तुम्हारे शरीर सहित बचा लेंगे ताकि तुम अपने बाद आने वालों के लिए एक निशानी बनो। और निस्संदेह बहुत से लोग हमारी निशानियों से असावधान हैं।} [यूनुस: 92]
उस आयत का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह इस हद तक हिल गया कि वह दर्शकों के सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया: "मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और मैं इस कुरान पर विश्वास करता हूं।"
मौरिस बुकेले का योगदान
मौरिस बुकेले उस चेहरे से बिल्कुल अलग चेहरा लेकर फ्रांस लौटे, जो उनके साथ गया था। वे वहाँ दस साल तक रहे, और उनके मन में बस यही था कि वे नए खोजे गए वैज्ञानिक तथ्यों का पवित्र क़ुरआन से कितना मेल खाते हैं, और क़ुरआन में कही गई बातों में एक भी वैज्ञानिक विरोधाभास ढूँढ़ते रहें। इसके बाद उन्हें अल्लाह के इस कथन का नतीजा मिला: {झूठ न तो उसके आगे से आता है और न पीछे से। वह तो अत्यन्त तत्वदर्शी, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर की ओर से उतारा जाता है।} [फ़ुस्सिलात: 42]
फ्रांसीसी विद्वान मौरिस बुकेले द्वारा बिताए गए इन वर्षों का फल पवित्र कुरान पर एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन था जिसने पश्चिमी देशों और उनके विद्वानों को अंदर तक झकझोर दिया। पुस्तक का शीर्षक था: "कुरान, तोरा, बाइबिल और विज्ञान: आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन।" तो इस पुस्तक ने क्या हासिल किया?!
पहली छपाई के साथ ही, यह सभी किताबों की दुकानों में बिक गई! फिर इसकी मूल भाषा (फ़्रेंच) से अरबी, अंग्रेज़ी, इंडोनेशियाई, फ़ारसी, तुर्की और जर्मन में अनुवाद के बाद इसे लाखों की संख्या में पुनर्मुद्रित किया गया। इसके बाद यह पूर्व और पश्चिम के सभी किताबों की दुकानों में फैल गई, और अब आप इसे अमेरिका में किसी भी युवा मिस्र, मोरक्को या खाड़ी नागरिक के हाथों में पा सकते हैं।
जिन यहूदी और ईसाई विद्वानों के दिल और आँखें ईश्वर ने अंधी कर दी हैं, उन्होंने इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने केवल तर्क-वितर्क और शैतान की फुसफुसाहट से प्रेरित हताशापूर्ण प्रयास ही लिखे हैं। उनमें से अंतिम थे डॉ. विलियम कैंपबेल, जिन्होंने अपनी पुस्तक "इतिहास और विज्ञान के प्रकाश में कुरान और बाइबिल" लिखी। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की यात्रा की, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम में कुछ विद्वानों ने इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया तैयार करना शुरू कर दिया, और जब वे इसे पढ़ने में अधिक तल्लीन हो गए और इस पर अधिक विचार करने लगे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और सार्वजनिक रूप से विश्वास की दो गवाहियाँ दीं!!
मौरिस बुकेले के कथनों से
मौरिस बुकेल अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में कहते हैं: "कुरान के इन वैज्ञानिक पहलुओं ने मुझे शुरू में बहुत आश्चर्यचकित किया। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि तेरह शताब्दियों से भी पहले लिखे गए एक ग्रंथ में, इतनी सटीकता से, इतने विविध विषयों पर इतनी बड़ी संख्या में विषयों की खोज करना और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के पूर्णतः अनुरूप बनाना संभव है!!"
वह यह भी कहते हैं: "मैंने सबसे पहले पवित्र कुरान का अध्ययन बिना किसी पूर्वधारणा के और पूरी निष्पक्षता के साथ किया, ताकि कुरान के पाठ और आधुनिक विज्ञान के आंकड़ों के बीच सहमति की डिग्री का पता लगाया जा सके। मैं जानता था - इस अध्ययन से पहले, और अनुवादों के माध्यम से - कि कुरान में कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन मेरा ज्ञान सीमित था।
अरबी पाठ के गहन अध्ययन के फलस्वरूप, मैं एक सूची तैयार कर पाया। इसे पूरा करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि कुरान में ऐसा कोई कथन नहीं है जिसकी आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से आलोचना की जा सके। उसी निष्पक्षता के साथ, मैंने पुराने नियम और सुसमाचारों का भी यही परीक्षण किया।
जहां तक पुराने नियम का प्रश्न है, तो पहली पुस्तक, उत्पत्ति से आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां ऐसे कथन थे जिनका हमारे समय के सर्वाधिक स्थापित वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता था।
जहाँ तक सुसमाचारों का प्रश्न है, हम पाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का पाठ स्पष्ट रूप से लूका रचित सुसमाचार का विरोधाभासी है, और लूका रचित सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा प्रस्तुत करता है जो पृथ्वी पर मनुष्य की प्राचीनता के संबंध में आधुनिक ज्ञान से सहमत नहीं है।”
डॉ. मौरिस बुकेले भी कहते हैं: "क़ुरान के पाठों से पहली बार रूबरू होने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले जो बात आती है, वह है इसमें वर्णित वैज्ञानिक विषयों की प्रचुरता। हालाँकि हमें वर्तमान टोरा में भारी वैज्ञानिक त्रुटियाँ मिलती हैं, लेकिन क़ुरान में हमें कोई त्रुटि नहीं मिलती। अगर क़ुरान का लेखक कोई इंसान होता, तो वह सातवीं शताब्दी में ऐसे तथ्यों के बारे में कैसे लिख सकता था जो उसके समय से संबंधित नहीं थे?!"
1988 में, फ्रेंच अकादमी ने उन्हें उनकी पुस्तक, द होली कुरान एंड मॉडर्न साइंस के लिए इतिहास पुरस्कार से सम्मानित किया।
अमेरिकी वैज्ञानिक जेफरी लैंग
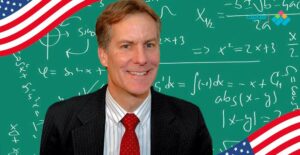 इसका परिचय
इसका परिचय
अमेरिकी गणितज्ञ जेफरी लैंग का जन्म 1954 में ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट में हुआ था। उन्होंने पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में कैनसस विश्वविद्यालय में गणित विभाग में प्रोफेसर हैं।
ईसाई धर्म को अस्वीकार करना
अपनी पुस्तक, द स्ट्रगल फॉर फेथ में जेफरी लैंग ने अपने रोमांचक अनुभव का वर्णन किया है, जो लोगों को पश्चिम में इस्लाम के प्रसार और यह कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है।
वह व्यक्ति एक ईसाई परिवार में पला-बढ़ा था, और जब उसके धर्म के प्रोफेसर गणित के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, तो हाई स्कूल के एक छात्र, जेफरी लैंग ने उन पर हमला कर दिया और सबूतों को लेकर उनसे बहस की। प्रोफेसर उससे नाराज़ हो गया और उसे चेतावनी देकर कक्षा से निकाल दिया।
युवक घर लौट आया और जब उसके माता-पिता ने यह कहानी सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए और बोले: बेटा, तुम नास्तिक हो गए हो।
लैंग कहते हैं, "दरअसल, पश्चिमी ईसाई धर्म में उनकी आस्था खत्म हो गई थी।" लैंग दस साल तक नास्तिकता की इसी अवस्था में रहे, खोज करते रहे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी यूरोप के लोगों की समृद्ध ज़िंदगी के बावजूद झेलने वाली बदहाली से हुई।
उनके इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
पल भर में, यह आश्चर्य क़ुरान से आया, जो एक सऊदी परिवार से एक उपहार था। लैंग क़ुरान का वर्णन करते हुए कहते हैं:
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर के सामने खड़ी हूँ जो मेरी सारी छिपी हुई भावनाओं पर रोशनी डाल रहा है। मैं कुछ समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रही थी, और मैंने पाया कि वो मेरे इंतज़ार में बैठा है, मेरे अंदर गहराई तक उतर रहा है और मुझे सच्चाई से रूबरू करा रहा है।
इसलिए, नास्तिक होने के बाद उन्होंने 1980 ई. में इस्लाम धर्म अपना लिया।
शॉकी फुटाकी...जापानी डॉक्टर
 शौकी वोताकी का इस्लाम धर्म अपनाना जापान के इतिहास में, और वास्तव में पूरे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कैसे? और जापानी डॉक्टर शौकी वोताकी के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है? शौकी वोताकी... जापानी डॉक्टर
शौकी वोताकी का इस्लाम धर्म अपनाना जापान के इतिहास में, और वास्तव में पूरे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कैसे? और जापानी डॉक्टर शौकी वोताकी के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है? शौकी वोताकी... जापानी डॉक्टर
वोताकी एक जापानी डॉक्टर हैं जिन्होंने सड़सठ साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और मिलनसार है, और वे अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले उनका धर्म बौद्ध धर्म था, और वे टोक्यो (जापान की राजधानी) के मध्य में स्थित एक बड़े अस्पताल के निदेशक थे। यह अस्पताल दस हज़ार लोगों की स्वामित्व वाली एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। डॉ. वोताकी ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद से ही घोषणा कर दी थी कि वे दस हज़ार शेयरधारकों को इस्लाम धर्म में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
अस्पताल निदेशक के रूप में अपने कार्य के अलावा, डॉ. फुटाकी 1954 में सेकामी जिब नामक एक जापानी मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक भी थे। जापान पर गिराए गए परमाणु बम और उसके प्रभाव के मुद्दे में उनकी रुचि थी और उन्होंने इसके लिए दान एकत्र करने का प्रयास किया। जब वे इसमें असफल रहे, तो उन्होंने दस जापानी कंपनियों से साठ करोड़ जापानी येन की जबरन वसूली की, क्योंकि उन्होंने उनके हितों को प्रभावित करने वाली गुप्त जानकारी प्रकाशित करने की धमकी दी थी। एक लंबी सुनवाई के बाद, उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और उनका चिकित्सा लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
शौकी फ़ुताकी के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
इस्लाम से उनका पहला परिचय जेल में प्रवेश के बाद हुआ, और उन्होंने कई दार्शनिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू कीं। एकेश्वरवाद का विचार उनके भीतर गहराई से घर करने लगा, और यह विचार उनके भीतर तब गहराई से जड़ें जमा चुका था जब उन्होंने कई इस्लामी हस्तियों से संपर्क किया, जिनमें जापान मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अबू बकर मोरिमोटो नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल थे, जो उनसे कहा करते थे: "दुनिया में जितने ज़्यादा मुसलमान होंगे, धरती पर उत्पीड़ितों की समस्या उतनी ही कम होगी, क्योंकि इस्लाम प्रेम और भाईचारे का धर्म है।"
जब फुटाकी को इस्लाम में मार्गदर्शन मिला, तो उन्होंने, उनके बेटे और एक अन्य मित्र ने इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया और टोक्यो के इस्लामिक सेंटर में अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की।
शौकी फुटाकी का योगदान
शौकी फुटाकी का इस्लाम धर्म अपनाना पूरे जापान के इस्लाम धर्म अपनाने का संकेत है! लेकिन उनके धर्म परिवर्तन को जापान में एक बड़ा परिवर्तन क्यों माना जा रहा है?
क्योंकि इस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म अपनाने के तुरंत बाद, पूरे जापान में इस्लाम फैलाने की अपनी मंशा ज़ाहिर की थी। मार्च 1975 में इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, उन्होंने टोक्यो मस्जिद में अड़सठ लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने इस्लामिक ब्रदरहुड एसोसिएशन की भी स्थापना की।
इसके अलावा, 4 अप्रैल, 1975 को टोक्यो मस्जिद में दो सौ जापानी लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की। इस प्रकार, डॉ. शौकी फुटाकी ने अपने जापानी भाइयों को बड़ी संख्या में ईश्वर के धर्म में प्रवेश कराने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, और अंततः इन नए मुसलमानों से, जिस इस्लामिक ब्रदरहुड एसोसिएशन का वे नेतृत्व कर रहे थे, उसके सदस्यों की संख्या लगभग बीस हज़ार जापानी मुसलमानों तक पहुँच गई, और यह सब एक वर्ष से भी कम समय में हुआ।
इसलिए, शौकी फुटाकी का इस्लाम में धर्मांतरण जापान के इतिहास में और वास्तव में पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।
हालाँकि, अरबी भाषा में पारंगत न होने और मुस्लिम देशों में न रहने वालों में एक ऐसी प्रवृत्ति उभरी है जो अज्ञानता के प्रभाव से उपजी कुछ अशुद्धियाँ हैं; डॉ. शौकी फ़ुताकी अपने इस्लामिक सोसाइटी के सदस्यों के नए मुसलमानों के साथ सूअर का मांस और शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने के मामले में नरम थे, शायद उनकी अज्ञानता का कोई बहाना था, और शायद वह उन्हें धीरे-धीरे अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसलिए, इस्लामी देशों - और उनमें सबसे प्रमुख अरब देशों - को इन देशों में प्रचारक भेजने चाहिए (2)।
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
डगलस आर्चर
जमैका में शैक्षिक संस्थान के निदेशक डॉ. डगलस आर्चर के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी। डॉ. डगलस आर्चर के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है? धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या योगदान दिया? डगलस आर्चर... इस्लाम एक अनोखा धर्म है।
डगलस आर्चर, जिनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला था, जमैका में शैक्षिक संस्थान के निदेशक थे। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले, वे सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट थे और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में भी काम किया था।
डगलस आर्चर के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
इस्लाम के साथ उनकी कहानी तब शुरू हुई जब वे विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पर व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ कुछ मुस्लिम छात्र थे, और वे अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते थे। व्याख्यान के बाद उन्हें उनके साथ बैठना पड़ता था। इन मुलाकातों के दौरान, उनके विश्वासों और सिद्धांतों के बारे में और जानने की उनकी जिज्ञासा और इच्छा जागृत हुई, और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए।
इस्लाम की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने वाली महत्वपूर्ण चीजों में से एक था दर्शनशास्त्र का अध्ययन, जिसके माध्यम से उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ बातें पढ़ीं।
एक और बात जिसने उन्हें इस्लाम को और करीब से जानने में मदद की, वह थी पास में रहने वाला एक सऊदी स्नातक छात्र, जो उनसे इस्लाम के बारे में खूब बातें करता था। उसने उसे कई इस्लामी किताबें दीं और विश्वविद्यालय के दो मुस्लिम प्रोफेसरों से भी मिलवाया।
जहां तक उस महत्वपूर्ण बिंदु का प्रश्न है जिसके कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, तो वे कहते हैं:
"एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा डॉक्टरेट शोध शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण पर था, और वहाँ से मैंने सीखा कि राष्ट्रों को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या चाहिए। मैंने पाया कि इस्लाम के मूल स्तंभ राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण के लिए एक मज़बूत आधार और मूल्यवान आधार प्रदान करते हैं। इसलिए, अगर आप मुझसे पूछें: मैंने इस्लाम क्यों अपनाया? तो मैं आपको बताऊँगा: क्योंकि इस्लाम एक अनूठा धर्म है, जिसके मूल स्तंभ शासन का आधार बनते हैं जो इसके अनुयायियों के विवेक और जीवन, दोनों का मार्गदर्शन करता है।"
डगलस आर्चर का योगदान
डगलस आर्चर ने इस्लाम का बचाव करते हुए कहा कि यह पूँजीवाद और साम्यवाद के तहत रहने वालों की समस्याओं को सुलझाने और उनकी सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ये दोनों व्यवस्थाएँ मानवता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहीं, लेकिन इस्लाम दुखी लोगों को शांति और भ्रमित व भटके हुए लोगों को आशा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
डॉ. डगलस आर्चर, कैरेबियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पद के दौरान, संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से वेस्ट इंडीज में इस्लाम का प्रसार करने का भी प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने इस्लामी उद्देश्य के समर्थन में सऊदी अरब और कुवैत का भी दौरा किया है।
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
डेविड लाइवली
 अमेरिकी डेविड लाइवली के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी, जिसका मन और हृदय ईसाई धर्म के दो मुख्य सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सका: त्रिदेव का सिद्धांत और मोक्ष का सिद्धांत। तो डेविड के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है?
अमेरिकी डेविड लाइवली के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी, जिसका मन और हृदय ईसाई धर्म के दो मुख्य सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सका: त्रिदेव का सिद्धांत और मोक्ष का सिद्धांत। तो डेविड के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है?
डेविड लाइवली का जन्म फिलाडेल्फिया, पेन्सिलवेनिया में हुआ था, और उन्होंने लेह विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने तक गणित का अध्ययन किया।
वह अपने बारे में कहते हैं: "अपनी युवावस्था के शुरुआती दिनों में, मैं और मेरा परिवार प्रोटेस्टेंट चर्च में नियमित रूप से जाते थे, और प्रोटेस्टेंटवाद अधिकांश अमेरिकी लोगों का धर्म है। मैंने शुरू से ही धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं का अध्ययन किया, लेकिन मैंने देखा कि मेरा मन और हृदय दो बुनियादी ईसाई मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर रहा था, जो हैं:
त्रिएकत्व का सिद्धांत (किसी भी रूप में अस्वीकृत) क्योंकि यह तर्क का खंडन करता है।
- मोक्ष का सिद्धांत मसीह को दिया गया है, शांति उस पर हो, क्योंकि इसमें नैतिकता के क्षेत्र में धार्मिक विरोधाभास शामिल हैं।
फिर मैंने एक नया विश्वास खोजने का प्रयास किया जो मुझे भटकाव और हानि से बचा सके, तथा उस आध्यात्मिक शून्य को भर सके जिससे अमेरिकी और यूरोपीय युवा पीड़ित थे और जिसके बारे में शिकायत कर रहे थे।
डेविड लाइवली के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
डेविड लाइवली अपने बारे में बताते हुए कहते हैं:
"मेरी मुलाक़ात एक अमेरिकी दोस्त से हुई जो मुझसे पहले इस्लाम धर्म अपना चुका था, और उसके पास पवित्र क़ुरआन के अर्थों का अंग्रेज़ी में अनुवाद था। मैंने इसे अपनी धार्मिक पुस्तकों के संग्रह में शामिल करने के लिए ले लिया। जैसे ही मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के सिद्धांतों से मेरा दिल सहज हो गया। फिर मैंने इस्लाम की ओर रुख़ किया और ख़ुदा से ये दुआएँ कीं: ऐ मार्गदर्शन के स्वामी, अगर यह इस्लाम नाम का धर्म तेरा सच्चा धर्म नहीं है जो तुझे रास आए, तो मुझे इससे और मेरे मुसलमान साथियों से दूर कर दे। अगर यह तेरा सच्चा धर्म है, तो मुझे इसके क़रीब ले आ और मुझे इसकी ओर मार्गदर्शन कर।"
एक हफ़्ता भी नहीं बीता था कि इस्लाम मेरे दिल में बस गया और मेरे ज़मीर में मज़बूती से जड़ जमा गया। मेरे दिल और दिमाग़ को तसल्ली मिली, मेरी रूह को सुकून मिला, और मुझे इस बात का सुकून मिला कि इस्लाम सचमुच ख़ुदा का मज़हब है, और क़ुरआन भी सच कहता है: "बेशक ख़ुदा के नज़दीक दीन इस्लाम है" (अल इमरान: 19)।
डेविड लाइवली का योगदान
दाऊद अब्दुल्ला अल-तौहीदी (इस्लाम धर्म अपनाने के बाद यह उनका नाम था) ने मुसलमानों को उनकी स्थिति के प्रति सचेत करने का प्रयास किया तथा उनसे अपनी स्थिति बदलने का आग्रह करते हुए कहा:
इस्लाम और उसके उत्कृष्ट मूल्यों, नैतिकता और विश्वासों, और मुसलमानों की अपनी आस्था के प्रति अज्ञानता, अपने मूल्यों के ह्रास और इस्लाम के मूल्यों व नैतिकता से उनकी दूरी के बीच कितना अंतर है! मुस्लिम शासक इस्लाम के लिए काम करने में धीमे रहे हैं, हालाँकि यह उनका उत्कृष्ट संदेश है। इस्लामी विद्वानों ने इस्लाम की ओर आह्वान करने, इज्तिहाद करने और निर्णय देने में अपनी वास्तविक भूमिका को त्याग दिया है। इस्लामी विद्वानों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल विरासत के संरक्षण से संतुष्ट न हों, बल्कि उन्हें इस्लामी विचारों को व्यवहार में लाना होगा। तभी नबूवत, ईमान, अमल और दूसरों के लाभ का प्रकाश उनके पास लौटेगा।
यह आश्चर्यजनक है कि इस्लामी दुनिया में कितने युवा इस्लाम के आध्यात्मिक मूल्यों से दूर हो गए हैं और इसकी शिक्षाओं से दूर हो गए हैं, जबकि हम पश्चिमी दुनिया के युवाओं को इन मूल्यों के लिए प्यासे पाते हैं, लेकिन उन्हें अपने धर्मनिरपेक्ष समाजों में खोजने में असमर्थ पाते हैं, जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
जहां तक अमेरिकी मुस्लिम दाऊद अल-तौहीदी की इच्छा का प्रश्न है:
"मेरी इच्छा इस्लामी अध्ययन जारी रखने और तुलनात्मक धर्मों में विशेषज्ञता हासिल करने की है ताकि मैं अमेरिका में मुसलमानों की भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने, वहाँ बौद्धिक आक्रमण का सामना करने और गैर-मुसलमानों के बीच इस्लाम के प्रसार में योगदान दे सकूँ। मुझे यह भी उम्मीद है कि वह दिन आएगा जब मैं इस्लाम को अमेरिकी समाज के भविष्य के पुनर्निर्माण में प्रभावित करते हुए देखूँगा और दुनिया भर में इस्लाम के पुनर्जागरण में भाग लूँगा। इस्लाम किसी मातृभूमि को नहीं जानता, बल्कि यह सभी लोगों के लिए भेजा गया मार्गदर्शन है। पवित्र कुरान इस्लाम के रसूल के बारे में कहता है: {और हमने आपको, [हे मुहम्मद], संसार के लिए दया के अलावा कुछ नहीं बनाया है।} [अल-अंबिया: 107]
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
हंगेरियन वैज्ञानिक अब्दुल करीम जर्मेनियम
 इतिहास प्राच्यविद् (गुलागर मानियस) को हंगरी में इस्लाम अपनाने वाले प्रसिद्ध लोगों में से एक के रूप में याद रखेगा। हंगेरियन विद्वान अब्दुल करीम जर्मेनियम
इतिहास प्राच्यविद् (गुलागर मानियस) को हंगरी में इस्लाम अपनाने वाले प्रसिद्ध लोगों में से एक के रूप में याद रखेगा। हंगेरियन विद्वान अब्दुल करीम जर्मेनियम
इसका परिचय
गुलागर मानियस का जन्म 6 नवम्बर 1884 को हुआ था और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुल करीम जर्मनियस रख लिया था।
अब्दुल करीम जर्मेनियम, लॉरेंट एनोवॉक्स विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में, अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम और मुहम्मद के संदेश का प्रचार करने में सक्षम थे। विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर, बड़ी संख्या में लोग अब्दुल करीम जर्मेनियम के अनुयायी थे, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर अरब और इस्लामी इतिहास के लिए एक पीठ की स्थापना की।
उनके इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
डॉ. अब्दुल करीम जर्मनियस अपने इस्लाम धर्म अपनाने की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं: "एक बरसाती दोपहर थी, और मैं अभी किशोरावस्था में ही था, जब मैं एक पुरानी सचित्र पत्रिका के पन्ने पलट रहा था, जिसमें समसामयिक घटनाएँ काल्पनिक कहानियों के साथ मिश्रित थीं, जिनमें कुछ दूर-दराज़ देशों के विवरण भी थे। मैं कुछ देर उदासीनता से पन्ने पलटता रहा, जब अचानक मेरी नज़र एक उत्कीर्ण लकड़ी के पैनल पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींचा। यह चित्र सपाट छतों वाले घरों का था, जिनमें जगह-जगह गोल गुंबद थे जो अँधेरे आकाश में धीरे-धीरे ऊपर उठ रहे थे, और जिनके अँधेरे को अर्धचंद्राकार चाँद चीर रहा था।"
इस चित्र ने मेरी कल्पना को मोहित कर लिया, और मुझे उस चित्र में अंधकार पर विजय पाने वाले प्रकाश को जानने की एक अदम्य, अदम्य लालसा हुई। मैंने तुर्की, फिर फ़ारसी और फिर अरबी का अध्ययन शुरू किया, इन तीनों भाषाओं में निपुणता हासिल करने की कोशिश की ताकि मैं उस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकूँ जो मानवता में इस चकाचौंध भरे प्रकाश को फैलाती है।
गर्मियों की छुट्टियों में, मुझे बोस्निया जाने का सौभाग्य मिला—जो उनके देश के सबसे नज़दीकी पूर्वी देश था। जैसे ही मैंने होटल में चेक-इन किया, मैं मुसलमानों की गतिविधियों को देखने के लिए दौड़ पड़ा। मेरे मन में एक ऐसी धारणा बनी जो उनके बारे में अक्सर कही जाने वाली बातों से बिल्कुल उलट थी। मुसलमानों से यह मेरी पहली मुलाक़ात थी। यात्रा और अध्ययन से भरे जीवन में कई साल बीतते गए, और जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरी आँखें अद्भुत और नए क्षितिजों की ओर खुलती गईं।
ईश्वर की दुनिया में अपनी लंबी यात्राओं, एशिया माइनर और सीरिया की प्राचीन कलाकृतियों को देखने के आनंद, अनेक भाषाओं के ज्ञान और विद्वानों की पुस्तकों के हज़ारों पन्ने पढ़ने के बावजूद, उन्होंने यह सब बारीकी से पढ़ा। वे कहते हैं, "इन सबके बावजूद, मेरी आत्मा प्यासी रही।"
जब वे भारत में थे, एक रात उन्होंने देखा—जैसा कि कोई स्वप्न में देखता है—ईश्वर के दूत मुहम्मद (ईश्वर उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे) ने करुणामय स्वर में उनसे कहा: "यह उलझन क्यों? आगे का सीधा मार्ग पृथ्वी की सतह की तरह सुरक्षित और समतल है। दृढ़ कदमों और विश्वास की शक्ति के साथ चलो।" अगले शुक्रवार को, दिल्ली की शुक्रवारी मस्जिद में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की।
हज अब्दुल करीम जर्मनोस उन भावुक पलों को याद करते हुए कहते हैं: “वह जगह भावनाओं और उत्साह से भरी हुई थी, और मुझे याद नहीं कि उस समय क्या हुआ था। लोग मेरे सामने खड़े थे, मुझे गले लगा रहे थे। कितने ही बेचारे, थके हुए लोग मेरी ओर विनती भरी निगाहों से देख रहे थे, मुझसे दुआ मांग रहे थे और मेरा सिर चूमना चाहते थे। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये मासूम आत्माएं मुझे इस तरह न देखें जैसे मैं उनसे ऊँचे दर्जे का हूँ, क्योंकि मैं धरती के कीड़ों के बीच एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं हूँ, या प्रकाश की तलाश में भटका हुआ एक व्यक्ति, अन्य दुखी प्राणियों की तरह असहाय और शक्तिहीन। इन अच्छे लोगों की कराह और आशाओं के सामने मैं शर्मिंदा था। अगले दिन और उसके बाद के दिन, लोग मुझे बधाई देने के लिए समूहों में मेरे पास आए, और मुझे उनके प्यार और स्नेह से इतना मिला कि मैं अपने बाकी जीवन के लिए भोजन जुटा सका।
भाषा सीखने के प्रति उनका जुनून
अब्दुल करीम जर्मनस ने पश्चिमी भाषाएँ: ग्रीक, लैटिन, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इतालवी और हंगेरियन, और पूर्वी भाषाएँ: फ़ारसी और उर्दू सीखीं। उन्होंने अपने शिक्षकों: वैम्बरी और गोल्डज़िहर, जिनसे उन्हें इस्लामी पूर्व के प्रति जुनून विरासत में मिला था, के अधीन अरबी और तुर्की भाषा में भी निपुणता हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1905 के बाद इस्तांबुल और वियना विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 1906 में ओटोमन साहित्य पर जर्मन में एक किताब और सत्रहवीं शताब्दी में तुर्किक वर्गों के इतिहास पर एक और किताब लिखी, जिसके लिए उन्हें एक पुरस्कार मिला जिससे उन्हें लंदन में लंबा समय बिताने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में अपनी पढ़ाई पूरी की।
1912 में वे बुडापेस्ट लौट आए, जहां उन्हें ओरिएंटल हाई स्कूल में अरबी, तुर्की और फारसी भाषाओं और इस्लामी इतिहास और संस्कृति का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, फिर आर्थिक विश्वविद्यालय के ओरिएंटल विभाग में, और फिर 1948 में बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में अरबी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने अरबी, इस्लामी सभ्यता का इतिहास और प्राचीन और आधुनिक अरबी साहित्य पढ़ाना जारी रखा, इस्लामी राष्ट्रों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण के बीच संबंध खोजने की कोशिश की, जब तक कि वे 1965 में सेवानिवृत्त नहीं हो गए।
भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें इस्लामी इतिहास के प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए भारत आमंत्रित किया, इसलिए उन्होंने दिल्ली, लाहौर और हैदराबाद (1929-1932 ई।) के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। वहाँ, उन्होंने दिल्ली की महान मस्जिद में इस्लाम में अपने धर्मांतरण की घोषणा की, शुक्रवार का उपदेश दिया और नाम (अब्दुल करीम) धारण किया। वह काहिरा गए और अल-अजहर के शेखों के साथ इस्लाम के अध्ययन में जुट गए, फिर एक तीर्थयात्री के रूप में मक्का गए, पैगंबर की मस्जिद का दौरा किया और अपनी तीर्थयात्रा के दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी: ईश्वर महान है, जो 1940 ई। में कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काहिरा और सऊदी अरब में वैज्ञानिक जांच (1939-1941 ई।) भी की, और उनके परिणामों को दो खंडों में प्रकाशित किया: अरबी साहित्य के मील के पत्थर (1952 ई
1955 के वसंत में, वे समकालीन अरब विचारों पर अरबी में व्याख्यान देने के लिए सरकार के निमंत्रण पर काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और दमिश्क में कुछ महीने बिताने के लिए वापस लौटे।
उनका योगदान
डॉ. अब्दुल करीम जर्मनोस ने अपने पीछे एक समृद्ध और विविध वैज्ञानिक विरासत छोड़ी है। उनकी रचनाओं में शामिल हैं: तुर्की भाषा के नियम (1925), तुर्की क्रांति और अरब राष्ट्रवाद (1928), आधुनिक तुर्की साहित्य (1931), इस्लाम में आधुनिक रुझान (1932), अरब प्रायद्वीप, सीरिया और इराक की खोज और आक्रमण (1940), अरब संस्कृति का पुनर्जागरण (1944), अरबी भाषाई संरचनाओं का अध्ययन (1954), इब्न अल-रूमी (1956), विचारकों के बीच (1958), पूर्व के प्रकाश की ओर, चयनित अरब कवि (1961), और इस्लामी संस्कृति और मगरेब का साहित्य (1964)। उन्होंने तीन पुस्तकें भी लिखीं: प्रवासन साहित्य, अरब यात्री और इब्न बतूता, और अरबी साहित्य का इतिहास।
इस हंगेरियन प्रोफेसर, जिनके अध्ययनों को पूरे अरब जगत में व्यापक मान्यता मिली, ने इस्लामी आह्वान के प्रसार और शेख अबू यूसुफ अल-मसरी के साथ मिलकर एक प्रसिद्ध इस्लामी पुस्तकालय की स्थापना में योगदान दिया। हंगेरियन सरकार ने इस पुस्तकालय में रुचि ली और आज भी इसे प्रायोजित कर रही है, इस्लामी विरासत और इतिहास को संरक्षित कर रही है और वहाँ के मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रही है।
समुद्र पार करके मिस्र की रोमांचक यात्रा के बाद, उन्हें 1939 में रेगिस्तान की यात्रा करने का अवसर मिला। उन्होंने लेबनान और सीरिया का दौरा किया और फिर अपनी दूसरी हज यात्रा की। अल्लाहु अकबर! के 1973 संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा: "मैंने अरब प्रायद्वीप, मक्का और मदीना की तीन बार यात्रा की, और मैंने अपनी पहली यात्रा के अनुभवों को अपनी पुस्तक अल्लाहु अकबर में प्रकाशित किया!" 1939-1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद, मैंने खतरों और थकान की परवाह किए बिना, एक नाविक के रूप में डेन्यूब नदी पार करके समुद्र तक पहुँचने का निश्चय किया। मैं मिस्र पहुँचा और वहाँ से अरब प्रायद्वीप के लिए रवाना हुआ। मैंने मदीना में कई महीने बिताए, जहाँ मैंने पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन से जुड़े स्थानों का दौरा किया: दो क़िबलाओं वाली मस्जिद के खंडहर, बाक़ी कब्रिस्तान, और बद्र व उहुद की लड़ाई के स्थल। मैं मदीना में मुहम्मद अली द्वारा स्थापित मिस्र की मस्जिद का मेहमान था। शाम को, मुस्लिम विद्वान दुनिया में इस्लाम की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुझसे मिलने आते थे। जैसा कि मैंने इस पुस्तक में बताया है, इस्लाम की भावना उनसे मुझ तक उसी शक्ति और गहराई के साथ पहुँचती थी, दुनिया भर में हो रहे तमाम सांसारिक बदलावों के बावजूद, बिना किसी कमी के, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी युवावस्था में, जो मैंने मुस्लिम पूर्व में बिताई थी, अनुभव किया था।" कारवां के साथ हिजाज़ से रियाद जाने का उनका सपना 1939 की यात्रा के दौरान साकार हुआ। वे चार कठिन हफ़्तों के बाद वहाँ पहुँचे, जिसका विवरण उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (अंडर द डिम लाइट ऑफ़ द क्रिसेंट) 1957 में अमर कर दिया।
अपनी बाद की पुस्तक, टुवर्ड्स द लाइट्स ऑफ़ द ईस्ट (1966) में, उन्होंने 1955 और 1965 के बीच अपनी यात्राओं के दौरान के अनुभवों को प्रस्तुत किया। इस अवधि के दौरान, वे मिस्र (1956), बगदाद (1962) और दमिश्क (1966) में अरब वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य बने। उन्होंने 1962 में बगदाद की स्थापना की 1200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री अब्दुल करीम कासिम के निमंत्रण पर बगदाद का दौरा किया। इसके बाद वे इराकी वैज्ञानिक अकादमी के सदस्य बने और उद्घाटन समारोह में "हंगरी में इस्लाम का इतिहास" शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1964 में, मिस्र सरकार ने उन्हें अल-अजहर की स्थापना की सहस्राब्दी के उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 1965 में, किंग फैसल बिन सऊद ने उन्हें मक्का में इस्लामिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने वहां रहते हुए, 81 वर्ष की आयु में तीसरी बार हज की रस्में निभाईं।
जर्मनस एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने विविध विषयों पर लेखन किया। उन्होंने ओटोमन तुर्कों के इतिहास और साहित्य पर लिखा, तुर्की गणराज्य के समकालीन विकास, इस्लाम और समकालीन इस्लामी बौद्धिक आंदोलनों, और अरबी साहित्य पर शोध किया। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक, अरबी साहित्य का इतिहास, 1962 में प्रकाशित हुई, और उससे पहले, 1961 में अरब कवियों का प्रकाशन हुआ। उन्होंने अरब भूगोलवेत्ताओं, लंदन 1954 में अरब यात्रियों और भूगोलवेत्ताओं के बारे में भी लिखा, और उन्होंने भारत पर कई अध्ययन लिखे। उन्होंने अपनी पुस्तकें और शोध हंगेरियन के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी और जर्मन जैसी कई भाषाओं में लिखे। शायद उनकी सहज, आकर्षक शैली ही उनकी पुस्तकों के प्रसार के पीछे थी। इस प्रकार, जर्मनस ने अरब संस्कृति और साहित्य, इस्लाम और सामान्य रूप से पूर्वी सभ्यता को प्रस्तुत करने में अग्रणी भूमिका निभाई, और हंगरीवासियों की आने वाली पीढ़ियाँ उनकी रचनाओं से परिचित हुईं और उन्हें पसंद करने लगीं।
उनकी मृत्यु
अब्दुल करीम जर्मनस का 7 नवंबर 1979 को छियानवे वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें बुडापेस्ट के एक कब्रिस्तान में इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया गया। एरेड स्थित हंगेरियन भौगोलिक संग्रहालय में इस हंगेरियन मुस्लिम यात्री और प्राच्यविद् का संपूर्ण अभिलेख रखा गया है।
एमिल ब्रिस डी'एवेन... सभ्यताओं और पुरावशेषों के विद्वान
मिस्र का अध्ययन करने वाले अपने समकालीन फ्रांसीसी पुरातत्वविदों में, पुरातत्वविद् एमिल प्रेसे डैफ्ने, मिस्र के ज्ञान के सबसे प्रभावशाली योगदानकर्ताओं में से एक थे। वे एक प्रतिष्ठित, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल फ़ारोनिक पुरावशेषों का पता लगाया, बल्कि इस्लामी सभ्यता के अध्ययन में भी अपनी रुचि का विस्तार किया। उनकी खोजों का साहस और उनके साहसिक कारनामों की निडरता उनकी गहरी अंतर्दृष्टि, गहन अवलोकन, व्यापक ज्ञान और सत्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का प्रमाण है।
उन्होंने पुरातत्व को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों से समृद्ध किया, जिसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक निरंतर प्रयास किया, इसके लिए उन्होंने अपने पदों के अलावा, विरासत में मिली एक बड़ी संपत्ति का त्याग किया, जब तक कि वे लेखों और अध्ययनों के अलावा चौदह पुस्तकें लिखने में सक्षम नहीं हो गए, जिनमें से सबसे प्रमुख उनकी पुस्तक (मिस्र की प्राचीन वस्तुएं और इतिहास के उदय से लेकर रोमन प्रभुत्व तक मिस्र की कला का इतिहास) और उनका विशाल विश्वकोश (सातवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के अंत तक मिस्र की प्राचीन वस्तुओं की वास्तविकता से अरब कला) है।
एमिल डेफेन के कारनामे और उपलब्धियां प्रशंसा और मान्यता के योग्य हैं, और कला इतिहास के प्रति उत्साही लोगों की स्मृतियों में उनका नाम चैम्पोलियन, मैरिएट और मास्पेरो के साथ चमकना चाहिए।
1829 में, ब्राइस डेविन इब्राहिम पाशा की सेवा में एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम करने आए, फिर खानकाह के स्टाफ स्कूल में स्थलाकृति के प्रोफेसर और पाशा के बेटों के शिक्षक के रूप में। हालाँकि, अपने अत्यधिक अहंकार, अहंकार और निंदनीय व्यवहार की निंदा के कारण, वह अक्सर अपने वरिष्ठों के साथ उत्तेजित और लापरवाह हो जाते थे, यहाँ तक कि उन पर हमला भी कर देते थे। इससे उनका क्रोध उन पर भड़क उठता था, और अंततः इस घटना के कारण गवर्नर उन पर क्रोधित हो जाते थे।
इंजीनियर जल्द ही एक प्राच्यविद् और मिस्र-विज्ञानी बन गए, और उन्होंने खुद को अरबी भाषा, उसकी बोलियों, उसके उच्चारण और चित्रलिपि को समझने में समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्हें अपनी स्वतंत्र क्षमता का एहसास हुआ, उन्होंने 1837 ई. में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक यात्री, खोजकर्ता और पुरातत्वविद् के रूप में अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी।
एमिल ब्राइस डेविन के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
एमिल ब्रिस डी'एवेन ने इस्लाम का गहन अध्ययन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने कुरान, इस्लाम के पैगंबर के जीवन और उनके संदेश के अध्ययन से की। उन्होंने बताया कि कैसे अरब केवल युद्धरत, संघर्षरत कबीले थे, लेकिन पैगंबर उन्हें एक एकजुट, सुसंगठित राष्ट्र में बदलने में सक्षम थे, जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े साम्राज्यों: फारसी साम्राज्य और बीजान्टिन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, और उन्हें मुस्लिम शासन के अधीन कर दिया।
इस्लाम धर्म अपनाने के कारण के बारे में वे कहते हैं:
उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून न्याय, सत्य, सहिष्णुता और क्षमा की विशेषता रखता है, तथा पूर्ण मानव भाईचारे का आह्वान करता है, सभी सद्गुणों का आह्वान करता है, तथा सभी बुराइयों का निषेध करता है, तथा इस्लामी सभ्यता एक मानवीय सभ्यता है जिसने कई शताब्दियों तक प्राचीन विश्व पर प्रभुत्व बनाए रखा।
एमिल डेविन ने इन सबका अध्ययन किया और पाया कि उनका दिल और दिमाग उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम इदरीस डेविन रख लिया। उन्होंने किसानी वेश धारण किया और ऊपरी मिस्र और डेल्टा में अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़े।
एमिल ब्रिसे डी'एवेन का योगदान
अरब लोग इस्लामी पुरातत्व के क्षेत्र में ब्राइस डेविन के प्रति अधिक ऋणी हैं, बजाय फ़ारोनिक पुरातत्व के क्षेत्र में।
सभ्यताओं और पुरातत्व के विद्वान, इदरीस दाफेन, फ़ारोनिक और इस्लामी सभ्यताओं को उनकी सुप्तावस्था से पुनर्जीवित करने और जीवंत एवं सुलभ मानवतावादी अरब कला को हमारे सामने वापस लाने में सक्षम थे। इस्लाम इस फ्रांसीसी मुस्लिम प्राच्यविद् का ऋणी है।
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
क्रिस्टोफर चामोंट
वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में जानने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम क्रिस्टोफर हैमोंट से बदलकर अहमद रख लिया।
लेकिन इस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? यह हम उनके धर्म परिवर्तन की कहानी के ज़रिए जानेंगे।
क्रिस्टोफर चामोंट के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
क्रिस्टोफर चामोंट के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी तब शुरू हुई जब उन्हें त्रिदेवों की कहानी पर संदेह होने लगा, जिसका ठोस स्पष्टीकरण उन्हें केवल पवित्र कुरान में ही मिला। उन्हें इस्लाम में वह सब मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने इसकी प्रकृति और महानता को समझा। उन्हें त्रिदेवों के बारे में वह सब मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, जब उन्होंने पवित्र कुरान में पढ़ा कि ईसा मसीह - उन पर शांति हो - ईश्वर के एक दूत थे, कि वह एक इंसान थे, और केवल एक ही ईश्वर है जो पूजा और आज्ञाकारिता के योग्य है।
इसके बाद, क्रिस्टोफर चामोंट ने अंग्रेजी में अनुवादित पवित्र कुरान और इस्लाम पर कुछ अनुवादित पुस्तकें पढ़कर इस्लाम के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। वह सऊदी अरब में कार्यरत थे, जिससे उन्हें विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मुसलमानों से मिलने-जुलने का अवसर मिला। इस बारे में वे कहते हैं:
"विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मुसलमानों के साथ मेरी बातचीत और उनके साथ हुई चर्चाओं का इस्लाम के बारे में मेरी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैंने खुद को इस्लामी धर्म के दर्शन के बारे में जानने के लिए प्रेरित पाया।"
इस प्रकार क्रिस्टोफर चामोंट ने इस्लाम को जाना, जिस सत्य की वह खोज कर रहे थे, उस तक पहुंचे और विश्व के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने उस पर कैसे पकड़ बनाए रखी।
क्रिस्टोफर चामोंट का योगदान
क्रिस्टोफर चामोंट ने मुसलमानों से अपने धर्म की शिक्षाओं पर अडिग रहने का आह्वान किया क्योंकि यही उनकी सफलता का कारण हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा:
"इस्लाम की शिक्षाएँ महान हैं। अगर मुसलमान इनका पालन करते, तो वे प्रगति, शक्ति और सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाते। हालाँकि, मुसलमान अंतर्मुखी होते हैं, जिसके कारण दूसरे उनसे श्रेष्ठ हैं, जबकि आरंभिक मुसलमान सभ्यता और वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के मार्ग पर सबसे पहले चलने वाले थे।"
क्रिस्टोफर चामोंट ने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम की शिक्षाएं प्रगति और उन्नति का मार्ग हैं, उनका पालन न करना मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण है, तथा मुसलमानों का अपनी उपासना पर पुनः लौटना ही उनकी प्रगति और सफलता का मार्ग है।
अहमद चामोंट ने भी इस्लाम के बारे में बात करते हुए कहा:
"इस्लाम वह धर्म है जो इंसान के मन से बात करता है और इस दुनिया और आख़िरत में खुशी पाने की नींव रखता है। यह एक सच्चाई है। मुझे इस्लाम में वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और इंसान की किसी भी समस्या का समाधान पवित्र क़ुरआन में मिल सकता है।"
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
प्राच्यविद् हुसैन रूफ...धर्म और समाजशास्त्र के विद्वान
अंग्रेज़ प्राच्यविद्, धार्मिक विद्वान और समाजशास्त्री, श्री रोव का जन्म 1916 में इंग्लैंड में ईसाई और यहूदी माता-पिता के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अपने माता-पिता के ईसाई और यहूदी धर्मों का अध्ययन करके की, फिर हिंदू धर्म और उसके दर्शन, विशेष रूप से उसकी आधुनिक शिक्षाओं, और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और उनकी तुलना कुछ प्राचीन यूनानी सिद्धांतों से की। इसके बाद उन्होंने कुछ आधुनिक सामाजिक सिद्धांतों और मतों का अध्ययन किया, विशेष रूप से महान रूसी विद्वान और दार्शनिक, लियो टॉल्स्टॉय के विचारों का।
प्राच्यविद् हुसैन रौफ़ के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
श्री रूफ की इस्लाम में रुचि और अध्ययन अन्य धर्मों और मान्यताओं की तुलना में देर से शुरू हुआ, हालाँकि वे कुछ अरब देशों में रहे थे। इस्लाम से उनका पहला परिचय रोडवेल द्वारा पवित्र कुरान के अनुवाद को पढ़कर हुआ था, लेकिन वे इससे प्रभावित नहीं हुए क्योंकि यह एक विश्वसनीय और ईमानदार अनुवाद नहीं था, जैसा कि कई अन्य अनुवादों के साथ हुआ था, जो अज्ञानता या शत्रुतापूर्ण इरादों से दूषित थे, और जो कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुए थे।
सौभाग्य से, उनकी मुलाक़ात एक सुसंस्कृत, सच्चे इस्लाम प्रचारक से हुई, जो इस्लाम के प्रति उत्साही थे और इसे लोगों तक पहुँचाने में सच्चे थे। उन्होंने उन्हें इस्लाम की कुछ सच्चाइयों से परिचित कराया और पवित्र कुरान के अर्थों के अनुवादित संस्करण की ओर निर्देशित किया, जिसका अनुवाद एक मुस्लिम विद्वान ने किया था। उन्होंने तर्क और बुद्धि पर आधारित एक स्पष्ट और विश्वसनीय व्याख्या प्रस्तुत की, साथ ही उन सच्चे अर्थों को भी स्पष्ट किया जिन्हें अंग्रेजी भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। उन्होंने उन्हें कुछ अन्य इस्लामी पुस्तकों की ओर भी निर्देशित किया जो सत्य और स्पष्ट प्रमाणों से युक्त हैं। इन सबने उन्हें इस्लाम की सच्चाई के बारे में एक बुनियादी समझ विकसित करने में मदद की, जिससे उनमें निष्पक्ष वैज्ञानिक स्रोतों के माध्यम से इसके, इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई।
कुछ इस्लामी समूहों के साथ उनके संबंधों और उनकी परिस्थितियों के गहन अध्ययन ने उनके व्यवहार और रिश्तों पर इस्लाम के प्रभाव की सीमा की पुष्टि की। इससे इस्लाम की महानता के बारे में उनके प्रारंभिक विचार की पुष्टि हुई और वे पूरे दिल से उसमें विश्वास करने लगे।
इस अंग्रेज प्राच्यविद् ने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया?
उन्होंने इस्लाम अपनाने के अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहा:
1945 में एक दिन, कुछ दोस्तों ने मुझे ईद की नमाज़ देखने और उसके बाद खाने के लिए आमंत्रित किया। यह मुसलमानों की उस अंतरराष्ट्रीय भीड़ को करीब से देखने का एक अच्छा मौका था, जिसमें किसी भी तरह की राष्ट्रीय या नस्लीय कट्टरता नहीं थी... वहाँ मेरी मुलाक़ात एक तुर्की राजकुमार से हुई और उसके बगल में कई बेसहारा लोग भी थे। वे सब खाना खाने बैठ गए। अमीरों के चेहरों पर आपको कोई बनावटी विनम्रता, दिखावा या समानता का दिखावा नहीं दिखा, जैसा कि एक गोरे आदमी के चेहरे पर अपने काले पड़ोसी से बात करते समय दिखाई देता है। आपको उनमें कोई ऐसा नहीं दिखा जो समूह से अलग हो गया हो या खुद को एक तरफ़ या दूर कोने में छिपा लिया हो। आपको उनमें वह हास्यास्पद वर्गीय भावना नहीं दिखी जो सदाचार के झूठे पर्दों के पीछे छिपी हो सकती है।
"मेरे लिए यह कहना पर्याप्त है कि सावधानीपूर्वक विचार और विचार-विमर्श के बाद, मैंने पाया कि दुनिया के अन्य सभी ज्ञात धर्मों का अध्ययन करने के बाद, बिना मेरा ध्यान आकर्षित किए, और उनमें से किसी से भी सहमत हुए बिना, मैं स्वतः ही इस धर्म में विश्वास करने के लिए प्रेरित हुआ।"
इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की नैतिकता, सहिष्णुता और उदारता की प्रशंसा की और सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष की समस्या को हल करने में इस्लाम की क्षमता की ओर इशारा करते हुए कहा:
"मैंने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की है, पूर्व और पश्चिम दोनों, और मुझे यह देखने का अवसर मिला है कि हर जगह अजनबी का किस तरह से स्वागत किया जाता है, और यह जानने का अवसर मिला है कि उसका सम्मान करना पहली बात कहां है जो दिमाग में आती है, और पहला रिवाज कहां है (उसकी जांच करना और उसकी मदद करने से मिलने वाले हित या लाभ के बारे में जानना), और मैंने गैर-मुस्लिमों में ऐसा कोई नहीं पाया जो अजनबी का स्वागत करने, उसके साथ गर्मजोशी से पेश आने, उसका सम्मान करने और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना या किसी भी लाभ की उम्मीद किए बिना उसके प्रति दयालु होने में उनके बराबर हो... आर्थिक दृष्टिकोण से, हम पाते हैं कि इस्लामी समूह ही एकमात्र ऐसे समूह हैं जिन्होंने अमीर और गरीब के बीच के अंतर को इस तरह से मिटा दिया है कि गरीबों को समाज की संरचना को उलटने और अराजकता और नफरत को भड़काने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।"
प्राच्यविद् हुसैन रौफ़ का योगदान
अंग्रेज़ मुस्लिम प्राच्यविद् हुसैन रौफ़ उन प्रमुख यूरोपीय सामाजिक शोधकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने धर्मों और सामाजिक सिद्धांतों का गहन और गहन अध्ययन किया। वे इस्लाम की महानता, उसके उत्कृष्ट उद्देश्यों और सिद्धांतों, समस्याओं को सुलझाने और व्यक्तियों व मानव समाजों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों का सामना करने की उसकी असाधारण क्षमता, और विभिन्न वातावरणों और सभ्यताओं के साथ, उनकी विविधता और भिन्नताओं के बावजूद, उसकी अद्भुत अनुकूलनशीलता से चकित थे।
इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, यह स्वाभाविक ही था कि वे इस धर्म की ओर लोगों को बुलाने की पहल करें, जिसने उनके दिल, दिमाग और भावनाओं पर कब्ज़ा कर लिया था, ताकि वे अपने साथी नागरिकों को इसके सहिष्णु सिद्धांतों और उच्च लक्ष्यों के बारे में बता सकें, साथ ही झूठ की बाढ़ का खंडन कर सकें और इस्लाम के दुश्मनों द्वारा इसके साथ लगाए गए भ्रम और झूठ के भवन को ध्वस्त कर सकें।
और अल्लाह तआला ने सच ही कहा जब उसने कहा: "और उस व्यक्ति से बेहतर बात कौन कर सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और नेक काम करे और कहे, 'वास्तव में, मैं मुसलमानों में से हूँ।'" (फ़ुस्सिलात: 33)
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
डॉ. हामेद मार्कस, जर्मन वैज्ञानिक और पत्रकार
कुरान की शैली से प्रभावित जर्मन विद्वान हामेद मार्कस के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी। हामेद मार्कस के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी क्या है? और धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा? जर्मन विद्वान और पत्रकार डॉ. हामेद मार्कस
बचपन से ही, जब भी मौका मिलता, मुझे इस्लाम का अध्ययन करने की गहरी इच्छा होती थी। जिस शहर में मैं पला-बढ़ा, वहाँ के पुस्तकालय में मैंने कुरान की एक अनुवादित प्रति ज़रूर पढ़ी। इसी संस्करण से गोएथे ने इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की थी।
मैं कुरान की शानदार बौद्धिक शैली से बहुत प्रभावित हुआ, जिसने इस्लामी शिक्षाओं को भी लागू किया। मैं उस महान, दृढ़ भावना से भी चकित था जो इन शिक्षाओं ने शुरुआती मुसलमानों के दिलों में जगाई और प्रज्वलित की।
फिर, बर्लिन में, मुझे मुसलमानों के साथ काम करने और बर्लिन के पहले इस्लामी संघ के संस्थापक और बर्लिन मस्जिद के संस्थापक द्वारा पवित्र कुरान पर दिए गए प्रेरक और प्रेरणादायक व्याख्यानों का आनंद लेने का अवसर मिला। इस अद्वितीय व्यक्तित्व के साथ वर्षों के व्यावहारिक सहयोग के बाद, जिसके दौरान मैंने उनकी आत्मा और भावना की गहराई को देखा, मैं इस्लाम में विश्वास करने लगा। मैंने इसके उदात्त सिद्धांतों में, जिन्हें मानवीय विचारों का शिखर माना जाता है, अपने विचारों के पूरक के रूप में देखा।
ईश्वर में आस्था इस्लामी आस्था का एक मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन यह ऐसे सिद्धांतों या सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता जो आधुनिक विज्ञान के विपरीत हों। इसलिए, एक ओर आस्था और दूसरी ओर विज्ञान के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यह निस्संदेह एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में एक अनूठा और महान लाभ है जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दिया है।
इस्लाम धर्म की एक और विशिष्ट विशेषता यह है कि यह केवल नीरस, सैद्धांतिक शिक्षाओं का एक समूह नहीं है जो आँख मूँदकर और जीवन के हाशिये पर काम करती हैं। बल्कि, यह एक व्यावहारिक व्यवस्था की माँग करता है जो मानव जीवन को आकार देती है। इस्लाम के नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने वाली बाध्यकारी शिक्षाएँ नहीं हैं, बल्कि वे निर्देश और दिशानिर्देश हैं जो संगठित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं।
जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए, मैं इस बात से अधिकाधिक आश्वस्त होता गया कि इस्लाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समूह के व्यक्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने का सर्वोत्तम मार्ग अपनाता है, तथा उन्हें एक मजबूत और ठोस बंधन में जोड़ता है।
यह धार्मिकता और सहिष्णुता का धर्म है। यह निरंतर अच्छाई का आह्वान करता है, उसे प्रोत्साहित करता है और सभी परिस्थितियों और अवसरों पर उसकी प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाता है।
स्रोत: पुस्तक (इस्लाम में परिवर्तित हुए पुरुषों और महिलाओं के साथ आस्था की यात्रा) अब्दुल रहमान महमूद द्वारा तैयार की गई।
विक्टोरियन युग में इस्लाम अपनाने वाले तीन सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश लोगों की कहानी
ब्रिटिश साम्राज्य के चरम पर, ब्रिटेनवासियों ने ईसाई धर्म त्यागकर इस्लाम अपनाने का फैसला किया। बीबीसी के अनुसार, यहाँ तीन ऐसे अग्रदूतों की कहानियाँ दी गई हैं जिन्होंने विक्टोरियन रीति-रिवाजों को उस समय चुनौती दी जब ईसाई धर्म ब्रिटिश पहचान का आधार था।
 विलियम हेनरी क्विलियम
विलियम हेनरी क्विलियम
अब्दुल्ला क्विलियम
वकील विलियम हेनरी क्विलियम की इस्लाम में रुचि तब उत्पन्न हुई जब उन्होंने 1887 में भूमध्य सागर में एक नौका पर मोरक्को के लोगों को प्रार्थना करते देखा।
क्विलियम ने कहा, "तेज़ हवाओं या जहाज़ के हिलने-डुलने से वे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। मैं उनके चेहरों और भावों से बहुत प्रभावित हुआ, जिनमें पूर्ण विश्वास और ईमानदारी झलक रही थी।"“.
टैंजियर में अपने प्रवास के दौरान धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद, क्विलियम, जो उस समय 31 वर्ष के थे, ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने नए धर्म को "उचित और तार्किक" बताया, और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह उनके विश्वासों के विपरीत नहीं है।“.
यद्यपि इस्लाम धर्म अपनाने वालों को अपना नाम बदलने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी क्विलियम ने अपने लिए “अब्दुल्ला” नाम चुना।“.
1887 में इंग्लैंड लौटने के बाद, वह धर्म के प्रचारक बन गये और ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रयासों के कारण पूरे ब्रिटेन में लगभग 600 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया।.
 1894 में, ओटोमन सुल्तान ने महारानी विक्टोरिया की स्वीकृति से क्विलियम को ब्रिटिश द्वीप समूह के शेख अल-इस्लाम की उपाधि प्रदान की।
1894 में, ओटोमन सुल्तान ने महारानी विक्टोरिया की स्वीकृति से क्विलियम को ब्रिटिश द्वीप समूह के शेख अल-इस्लाम की उपाधि प्रदान की।
क्विलियम ने उसी वर्ष लिवरपूल में देश की पहली मस्जिद भी स्थापित की, जिसे उस समय कई लोग "ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर" मानते थे।“.
महारानी विक्टोरिया, जिनके देश में ओटोमन साम्राज्य से भी ज़्यादा मुसलमान थे, उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने क्विलियम द्वारा लिखित "इस्लाम का धर्म" नामक एक पुस्तिका का अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने इस्लामी धर्म का सारांश प्रस्तुत किया था। इस पुस्तिका का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था।.
कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए छह अतिरिक्त प्रतियों का अनुरोध किया था, लेकिन अधिक ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा व्यापक समाज को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका मानना था कि इस्लाम हिंसा का धर्म है।.
1894 में, ओटोमन सुल्तान ने, महारानी विक्टोरिया की स्वीकृति से, क्विलियम को “ब्रिटिश द्वीप समूह में इस्लाम के शेख” की उपाधि प्रदान की, जो मुस्लिम समुदाय में उनके नेतृत्व को प्रतिबिंबित करती थी।.
लिवरपूल के कई निवासियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन उन्हें अपने धर्म के कारण नाराजगी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसमें धर्म की आधिकारिक मान्यता के बावजूद उन पर ईंटों, मल और खाद से हमला किया गया।.
क्विलियम का मानना था कि हमलावरों का “दिमाग इस तरह से धोया गया था कि उन्हें विश्वास हो गया कि हम बुरे हैं।”“.
क्विलियम को स्थानीय स्तर पर वंचित समूहों के साथ काम करने, ट्रेड यूनियनों की वकालत करने और तलाक कानून में सुधार के लिए जाना जाता था, लेकिन उनका कानूनी करियर तब ख़राब हो गया जब उन्होंने तलाक चाहने वाले एक मुवक्किल की मदद करने की कोशिश की।.
 क्विलियम वोकिंग में ब्रिटेन की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद की स्थापना में शामिल थे।
क्विलियम वोकिंग में ब्रिटेन की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद की स्थापना में शामिल थे।
पति के लिए एक जाल बिछाया गया, जो कथित तौर पर व्यभिचार कर रहा था, जो उस समय एक आम बात थी, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा और क्विलियम को काम से निलंबित कर दिया गया।.
शहर के मुसलमानों पर इस घोटाले के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने 1908 में लिवरपूल छोड़ दिया, और दक्षिण में हेनरी डी लियोन के नाम से पुनः प्रकट हुए, हालांकि क्विलियम की जीवनी लिखने वाले रॉन गीव्स के अनुसार, बहुत से लोग उन्हें जानते थे।.
यद्यपि उनका प्रभाव कम हो गया, फिर भी वे देश की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद, जो वोकिंग में बनी थी, की स्थापना में शामिल थे, तथा क्विलियम को 1932 में सरे में दफनाया गया।
लिवरपूल मस्जिद पर आज भी उनका नाम अंकित है।.
 लेडी एवलिन
लेडी एवलिन
एवलिन कोबोल्ड का हाथ
उच्च वर्ग के किसी सदस्य का इस्लाम के प्रति आकर्षित होना तथा मुस्लिम देशों की यात्रा से प्रेरित होना कोई अजीब बात नहीं थी।.
लेडी एवलिन मरे का जन्म एडिनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था, और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन स्कॉटलैंड और उत्तरी अफ्रीका के बीच बिताया।.
उसने लिखा: "मैंने वहाँ अरबी सीखी। मुझे अपनी नानी से बचकर अल्जीरियाई दोस्तों के साथ मस्जिदों में जाने में बहुत खुशी होती थी। मैं दिल से एक अनैच्छिक मुसलमान थी।"“.
एवलिन डनमोर पार्क में अपने परिवार की संपत्ति पर हिरणों का शिकार करती थीं और सैल्मन मछली पकड़ती थीं।.
उनके खोजी पिता, डनमोर के सातवें अर्ल, चीन और कनाडा सहित कई देशों की यात्राओं के शौकीन थे। उनकी माँ, जो बाद में महारानी विक्टोरिया की महिला-सेविका बनीं, भी एक उत्साही यात्री थीं।.
 लेडी एवलिन हज करने वाली पहली ब्रिटिश महिला थीं।
लेडी एवलिन हज करने वाली पहली ब्रिटिश महिला थीं।
लेडी एवलिन को अपने माता-पिता से यात्रा और भ्रमण का शौक विरासत में मिला था, और उनकी मुलाकात अपने पति, व्यवसायी जॉन कोबोल्ड से काहिरा, मिस्र में हुई थी।.
यह ज्ञात नहीं है कि लेडी एवलिन ने कब इस्लाम धर्म अपनाया। हो सकता है कि धर्म परिवर्तन का बीज बचपन की यात्राओं के दौरान ही बोया गया हो, लेकिन रोम में बिताई गई छुट्टियों और पोप से मुलाकात के बाद लेडी एवलिन का धर्म और भी मज़बूत हो गया।.
बाद में उन्होंने लिखा: “जब परम पावन ने अचानक मुझसे बात की और पूछा कि क्या मैंने कैथोलिक धर्म अपना लिया है, तो मैं एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई, फिर मैंने जवाब दिया, ‘मैं एक मुस्लिम हूं, और मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या असर हुआ, क्योंकि मैंने वर्षों से इस्लाम के बारे में नहीं सोचा था।’ यात्रा शुरू हुई, और मैंने धर्म को पढ़ने और उसका अध्ययन करने का संकल्प लिया।”“.
इतिहासकार विलियम वेसी, जिन्होंने लेडी एवलिन्स मेमोयर्स की भूमिका लिखी थी, ने कहा कि धार्मिक आध्यात्मिक पहलू ने कई धर्मांतरित लोगों को आकर्षित किया।.
 लेडी एवलिन, उनके पति जॉन कोबोल्ड और उनकी बेटी का चित्र।
लेडी एवलिन, उनके पति जॉन कोबोल्ड और उनकी बेटी का चित्र।
उन्होंने कहा कि वे “इस विश्वास का पालन करते हैं कि सभी प्रमुख धर्मों में एक उत्कृष्ट एकता है...उन सतही सांप्रदायिक विवरणों से दूर जो उन्हें विभाजित करते हैं।”“.
मध्य पूर्व में लेडी एवलिन के अरब दोस्त उन्हें "लेडी ज़ैनब" कहकर पुकारते थे। महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों में उनकी पहुँच थी और उन्होंने इस्लामी संस्कृति में "महिलाओं के प्रभावशाली प्रभाव" के बारे में लिखा था।.
65 वर्ष की आयु में उन्होंने हज की रस्में निभाईं और वह यह सम्पूर्ण रस्म निभाने वाली पहली ब्रिटिश महिला थीं।.
इससे उन्हें “अंतहीन रुचि और प्रशंसा” मिली, और उनकी कहानी बाद में “मक्का की तीर्थयात्रा” नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई।“.
केन्या की एक संक्षिप्त यात्रा के अलावा उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1963 में 95 वर्ष की आयु में इनवर्नेस के एक नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह निर्देश छोड़ा कि उनके अंतिम संस्कार में बैगपाइप बजाया जाए और उनकी कब्र पर कुरान की एक आयत, "प्रकाश की आयत" उत्कीर्ण की जाए।.
उन्होंने अपनी डायरी में लिखा: "मैंने हमेशा खुद से पूछा है कि मैंने कब और क्यों इस्लाम धर्म अपनाया।"“.
उन्होंने आगे कहा: "मेरा जवाब यह है कि मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि इस्लाम की सच्चाई मुझ पर कब प्रकट हुई।"“.
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से मुसलमान रही हूं।’’“.
 रॉबर्ट स्टेनली ने सत्तर वर्ष की आयु में इस्लाम धर्म अपना लिया।
रॉबर्ट स्टेनली ने सत्तर वर्ष की आयु में इस्लाम धर्म अपना लिया।
रॉबर्ट स्टेनली
विक्टोरियन मुस्लिम इतिहास में आमतौर पर समाज के उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व रहा है, जिनकी कहानियां बेहतर तरीके से संरक्षित हैं।.
लेकिन क्रिस्टीना लांगडेन, जिन्हें अपने पिता द्वारा परिवार वृक्ष पर शोध करने के बाद पता चला कि उनके दादा मुस्लिम थे, तथा जो लिखित दस्तावेज और डायरियां रखती हैं, कहती हैं: "सामान्यतः ऐसे संकेत मिलते हैं कि यह प्रथा मध्यम वर्ग में उभरी।"“.
1870 के दशक में रॉबर्ट स्टेनली एक श्रमिक वर्ग के किराना व्यापारी से मैनचेस्टर के निकट स्थित शहर स्टैलीब्रिज के कंजर्वेटिव मेयर बने।.
लॉन्गडेन, जिन्होंने उनके बारे में एक पुस्तक लिखी है, कहते हैं कि स्टेनली एक न्यायाधीश भी थे और उन्होंने अपने मालिकों की राय के अनुसार मतदान न करने के कारण बर्खास्त किये गये श्रमिकों के लिए एक कोष की स्थापना की थी।.
मैंने यह भी पाया कि वह लिवरपूल स्थित क्विलियम मस्जिद के समाचार पत्र में नियमित रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में लिखते थे।.
स्टेनली की मुलाकात क्विलियम से 1890 के दशक के अंत में हुई जब वह अपने राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो चुके थे, और वे घनिष्ठ मित्र बन गए।.
लॉन्गडेन कहते हैं, "रॉबर्ट क्विलियम से 28 साल बड़े थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके बीच पिता-पुत्र जैसा रिश्ता था।"“.
हालाँकि, उन्होंने सत्तर वर्ष की आयु तक इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और अपने लिए “राशिद” नाम चुना।“.
लॉन्गडेन अपने शोध के आधार पर मानती हैं कि उस समय स्टेब्रिज में "कोई और मुसलमान नहीं था"। बाद में स्टेनली मैनचेस्टर चले गए और 1911 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई।
उनके इस्लाम धर्म अपनाने की बात तब तक गुप्त रखी गयी जब तक कि 1998 में लोंगडेन परिवार को इसका पता नहीं चला।
संयोगवश, लांगडेन के भाई स्टीफन ने विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए मिस्र में अध्ययन करने के बाद 1991 में इस्लाम धर्म अपना लिया था, जबकि दादा स्टेनली के इस्लाम धर्म अपनाने की सच्चाई का पता सात साल पहले चला था।.
जब उन्होंने अपने दादा के धर्म परिवर्तन के बारे में सुना तो उन्होंने इसे "अद्भुत आश्चर्य" बताया।“.
उन्होंने कहा, "तथ्य यह है कि एक व्यक्ति ने ऐसे समय में मुसलमान बनने का फैसला किया, जब किसी के लिए कुछ अपरंपरागत करना अकल्पनीय था, जब आप बैठकर इसके बारे में सोचते हैं, तो हां, यह मैनचेस्टर है।" उन्होंने आगे कहा, "लोग खड़े होने और अपनी आस्था के बारे में बोलने से डरते नहीं हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक।"“.
मैल्कम एक्स, वह व्यक्ति जो खड़े-खड़े मर गया

इस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, ईश्वर के बाद, अश्वेत अमेरिकियों के बीच इस्लामी धर्म का प्रसार करने में महान योगदान दिया, उस समय जब अमेरिका में अश्वेत लोग अपने और गोरों के बीच नस्लीय भेदभाव से बुरी तरह पीड़ित थे। उन्हें हर तरह के अपमान और अपमान का सामना करना पड़ा, और उनसे यातना और हर तरह की घृणा का सामना करना पड़ा।
इस अशांत वातावरण में, उत्पीड़न और अपमान के सभी रूपों से भरा हुआ, मैल्कम एक्स का जन्म एक ऐसे पिता से हुआ जो एक चर्च में मंत्री थे और एक मां वेस्ट इंडीज से थी। जब वह छह साल का था, उसके पिता को गोरों ने मार डाला था, जब उन्होंने उसका सिर कुचल दिया और उसे एक इलेक्ट्रिक बस के रास्ते में डाल दिया जो तब तक उनके ऊपर से गुजरती रही जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। मैल्कम एक्स के परिवार की परिस्थितियाँ आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से तेज़ी से बिगड़ने लगीं। उन्होंने गोरों से मिलने वाले दान और सामाजिक सहायता पर रहना शुरू कर दिया, जो वे देने में धीमे थे। इन कठोर परिस्थितियों के साथ, मैल्कम एक्स की माँ को मनोवैज्ञानिक आघात लगा जो तब तक बढ़ता रहा जब तक उन्हें एक मानसिक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, जहाँ उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया। मैल्कम एक्स और उनके आठ भाई-बहनों ने अपने पिता और माँ दोनों को खोने का कड़वाहट का स्वाद चखा
इस बीच, मैल्कम एक्स ने पास के एक स्कूल में दाखिला ले लिया, जहाँ वह अकेला नीग्रो था। वह बुद्धिमान और मेधावी था, अपने सभी साथियों से बेहतर प्रदर्शन करता था। उसके शिक्षक उससे डरते थे, जिसके कारण वे उसे मानसिक और नैतिक रूप से तोड़ते थे, और उसका मज़ाक उड़ाते थे, खासकर जब वह कानून की पढ़ाई जारी रखना चाहता था। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर उसने स्कूल छोड़ दिया और नीग्रो के लिए उपयुक्त विभिन्न अपमानजनक नौकरियों में काम किया, एक रेस्टोरेंट में वेटर से लेकर ट्रेन में काम करने वाले, नाइट क्लबों में जूते पॉलिश करने वाले तक, जब तक कि वह एक प्रसिद्ध नर्तक नहीं बन गया, जिसकी ओर लोगों ने ध्यान दिलाया। फिर वह लापरवाही और घाटे की ज़िंदगी से मोहित हो गया, इसलिए उसने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसने जुए को अपनी कमाई का मुख्य स्रोत बना लिया, जब तक कि वह ड्रग्स का सेवन करने और यहाँ तक कि उनका कारोबार करने, और फिर घरों और कारों को चुराने की हद तक नहीं पहुँच गया। यह सब तब हुआ जब वह अभी इक्कीस साल का भी नहीं हुआ था, जब तक कि वह और उसके दोस्त पुलिस के हाथों नहीं पड़ गए। उन्होंने उसके विरुद्ध दस वर्ष की जेल की अत्यधिक सजा सुनाई, जबकि श्वेतों के लिए जेल की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं थी।
जेल में, मैल्कम एक्स ने धूम्रपान और सूअर का मांस खाना छोड़ दिया, और खुद को पढ़ने और सीखने के लिए इस हद तक समर्पित कर दिया कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर हजारों पुस्तकों को पढ़ डाला, इस प्रकार एक उच्च स्तर की संस्कृति स्थापित की जिसने उन्हें अपने व्यक्तित्व की कमियों को पूरा करने में सक्षम बनाया।
उस दौरान, मैल्कम एक्स के सभी भाइयों ने (श्री मुहम्मद एलिजा) नाम के एक व्यक्ति के हाथों इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसने दावा किया था कि वह ईश्वर का एक पैगम्बर है जो केवल अश्वेतों के लिए भेजा गया है!! उन्होंने मैल्कम एक्स को हर तरह से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की, जब तक कि वह इस्लाम धर्म नहीं अपना लिया। उसके नैतिक मूल्यों में सुधार हुआ, उसका व्यक्तित्व और निखर गया, और वह जेल के अंदर इस्लाम का आह्वान करने वाले धर्मोपदेशों और बहसों में भाग लेने लगा। आखिरकार उसे माफ़ कर दिया गया और रिहा कर दिया गया ताकि वह जेल के अंदर इस्लाम का आह्वान न करे।
मैल्कम एक्स उस इस्लाम राष्ट्र से ताल्लुक रखता था, जिसकी झूठी अवधारणाएँ और नस्लवादी बुनियादें इस्लाम के विपरीत थीं, हालाँकि उसने इसे एक चमकदार नारे के रूप में अपनाया था, जिससे वह बेखबर था। यह अश्वेत जाति के प्रति पक्षपाती था और उसने इस्लाम को केवल उसी तक सीमित कर दिया था, अन्य जातियों को बहिष्कृत कर दिया था, जबकि वे इस्लाम के सद्गुणी नैतिकता और उत्कृष्ट मूल्यों से संपन्न थे... यानी, उन्होंने इस्लाम का दिखावा तो किया, लेकिन उसके सार और मूल को त्याग दिया।
मैल्कम एक्स ने नेशन ऑफ इस्लाम में शामिल होना जारी रखा और अपने वाक्पटु भाषणों और सशक्त व्यक्तित्व से इसके सदस्यों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया। वह एक अटूट शक्ति, शक्ति, ऊर्जा और जोश की एक अटूट भुजा थे, जब तक कि वह इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कई लोगों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो गए।
मैल्कम एक्स हज करना चाहते थे, और जब उन्होंने यात्रा की, तो उन्होंने सच्चे इस्लाम को करीब से देखा, उसकी सच्चाई जानी, और उस नस्लवादी सिद्धांत की ग़लती का एहसास किया जिसे उन्होंने अपनाया और जिसका आह्वान किया था। इसलिए उन्होंने सच्चे इस्लामी धर्म को अपनाया, और खुद को (हज मलिक अल शबाज़) कहा।
जब वे लौटे, तो उन्होंने सच्चे इस्लाम के आह्वान में खुद को समर्पित कर दिया और इस्लाम राष्ट्र की भ्रामक और भ्रामक अवधारणाओं को सुधारने की कोशिश की। हालाँकि, उन्हें उनसे शत्रुता और घृणा का सामना करना पड़ा। उन्होंने उन्हें परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट और दृढ़ कदमों से चलते रहे, सच्चे इस्लाम का आह्वान करते हुए, जो सभी प्रकार के नस्लवाद को मिटा देता है।
अपने एक प्रभावशाली उपदेश में, जो वे लोगों को ईश्वर की ओर बुलाने के लिए देते थे, अत्याचारियों ने सत्य की आवाज़ को दबाने के अलावा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। जब वे मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके लंबे, दुबले शरीर पर सोलह विश्वासघाती गोलियाँ दागी गईं, और फिर उनका अंत हो गया। और कितना अच्छा अंत था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें क़यामत के दिन शहीदों में शामिल करें।
.
मुहम्मद अली क्ले
 मुहम्मद अली क्ले, जिन्हें "कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर" के नाम से जाना जाता है, का जन्म 17 जनवरी, 1942 को हुआ था। वह एक अमेरिकी नागरिक हैं, एक पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं, और आलोचनाओं के बावजूद, उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक और सभी के द्वारा प्रिय व्यक्ति माना जाता है।
मुहम्मद अली क्ले, जिन्हें "कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर" के नाम से जाना जाता है, का जन्म 17 जनवरी, 1942 को हुआ था। वह एक अमेरिकी नागरिक हैं, एक पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं, और आलोचनाओं के बावजूद, उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक और सभी के द्वारा प्रिय व्यक्ति माना जाता है।
उनका इस्लाम धर्म अपनाना
1964 में इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, उन्होंने अपना नाम, जिसे वे "कैसियस" के नाम से जानते थे, बदलकर "मुहम्मद अली" रख लिया, बिना "क्ले" (जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ मिट्टी होता है) के। उन्हें अपनी लोकप्रियता में आई कमी की परवाह नहीं थी, जो बढ़ती जा रही थी और लोगों का उनके प्रति प्रेम क्षितिज पर छा रहा था। इस्लाम उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। 1966 में, उन्होंने दुनिया को फिर से चौंका दिया जब मुहम्मद अली ने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा: "इस्लाम उन युद्धों को हराम करता है जो ईश्वर और उसके रसूल के लिए और इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए नहीं हैं।" उन्होंने घोषणा की, "मैं उनसे नहीं लड़ूँगा... क्योंकि उन्होंने मुझे नीग्रो नहीं कहा...???" इस कथन के कारण अमेरिकियों के बीच अपनी लोकप्रियता में आई कमी की उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सैन्य बल में भर्ती न होने का आरोप लगाया गया। उनका मुक्केबाजी का खिताब छीन लिया गया और उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ आए फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद, उन्होंने पूरे चार साल तक कोई मुकाबला नहीं लड़ा। अंततः उन्होंने यह अपील जीत ली और पुनः मुक्केबाजी रिंग में लौट आये।
मुक्केबाज़ी
उन्होंने 3 बार विश्व हैवीवेट चैम्पियनशिप हासिल की और अली ने कई ऐतिहासिक मैचों में भाग लिया, जिनमें से शायद सबसे प्रमुख तीन मैच थे, जिनमें से पहला सबसे मजबूत प्रतियोगी "जो फ्रेज़ियर" के साथ था और दूसरा "जॉर्ज फ़ोरमैन" के साथ जहाँ उन्होंने अपना खिताब वापस पाया जो उनसे सात साल से छीना गया था। "अली" अपनी अपारंपरिक लड़ाई शैली, तितली की तरह चकमा देने, मधुमक्खी की तरह हमला करने, कौशल और मुक्कों को सहने के साहस के लिए तब तक प्रतिष्ठित थे जब तक कि वे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नहीं हो गए। वह दुनिया के सबसे तेज़ पंच के मालिक हैं, जिसकी गति 900 किमी प्रति घंटा है। वह अपने द्वारा खेले जाने वाले मैचों से पहले अपनी बातचीत के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि वह मीडिया के बयानों पर बहुत अधिक निर्भर थे।
उनकी बीमारी
मुहम्मद अली को पार्किंसन रोग का पता चला था, फिर भी वे आज भी एक प्रिय खेल आइकन बने हुए हैं। अपनी बीमारी के दौरान, वे बेहद धैर्यवान रहे, क्योंकि वे हमेशा कहते थे कि ईश्वर ने उन्हें यह दिखाने के लिए परीक्षा ली कि वे महान नहीं हैं, बल्कि ईश्वर ही महान है।
उसको सम्मान दें
हॉलीवुड में एक बहुत प्रसिद्ध सड़क है जिसे "द वॉक ऑफ फेम" कहा जाता है क्योंकि वे सड़क पर अपने सभी प्रसिद्ध सितारों के नाम के साथ एक सितारा बनाते हैं।
जब उन्होंने मुस्लिम मुक्केबाज़ मुहम्मद अली क्ले को सड़क पर अपने नाम का एक सितारा लगाने की पेशकश की, तो उन्होंने मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सड़क पर अपने नाम का एक सितारा लगाने से इनकार क्यों किया?
उन्होंने उनसे कहा कि उनका नाम उस पैगम्बर का नाम है, जिन पर वह विश्वास करते हैं, "मुहम्मद, ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें," और उन्होंने जमीन पर "मुहम्मद" नाम लिखवाने से पूरी तरह इनकार कर दिया।
लेकिन उनकी महान लोकप्रियता और उनके एथलेटिक करियर के दौरान प्राप्त उल्लेखनीय सफलता के सम्मान में, हॉलीवुड ने "मुहम्मद अली" नाम वाले सितारे को अन्य प्रसिद्ध लोगों की तरह जमीन पर नहीं, बल्कि सड़क पर एक दीवार पर चित्रित करने का निर्णय लिया।
आज तक, मुहम्मद अली के अलावा किसी और हस्ती का नाम दीवार पर नहीं है। बाकी सभी हस्तियों के नाम ज़मीन पर हैं।
उनके धर्मार्थ कार्य
2005 में, मुहम्मद अली ने अपने गृहनगर लुइसविले में मुहम्मद अली सेंटर की स्थापना की, जहाँ वे वर्तमान में अपनी यादगार वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। यह केंद्र एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है जो शांति, सामाजिक समृद्धि, ज़रूरतमंदों की मदद और उन महान मूल्यों को बढ़ावा देता है जिनमें मुहम्मद अली क्ले विश्वास करते थे।
अब्दुल्ला अल-तर्जुमन
 अब्दुल्ला अल-मजोर्की, या अब्दुल्ला अल-मजोर्की, जिन्हें अब्दुल्ला अल-तर्जुमन के नाम से भी जाना जाता है, मेजरका में एक स्पेनिश ईसाई और एक प्रमुख पादरी थे। वे आठवीं शताब्दी हिजरी के महानतम ईसाई विद्वानों में से एक थे। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले उनका नाम एंसेलम टोरमेडा था। जब ईश्वर ने उनका हृदय खोला और उन्हें इस्लाम की ओर निर्देशित किया, तो उन्होंने स्वयं को अब्दुल्ला कहा, और उनके साथ तरजुमान की उपाधि जुड़ गई क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने ट्यूनिस के सुल्तान के लिए अनुवादक के रूप में काम किया। उन्होंने 823 हिजरी में अरबी में "तुहफत अल-अरीब फी अल-रद्द अला अहल अल-सलिब" नामक पुस्तक लिखी, जिसका बाद में फ्रेंच में अनुवाद किया गया और 1885 ई. में पेरिस की "धर्मों का इतिहास" पत्रिका में प्रकाशित किया गया।
अब्दुल्ला अल-मजोर्की, या अब्दुल्ला अल-मजोर्की, जिन्हें अब्दुल्ला अल-तर्जुमन के नाम से भी जाना जाता है, मेजरका में एक स्पेनिश ईसाई और एक प्रमुख पादरी थे। वे आठवीं शताब्दी हिजरी के महानतम ईसाई विद्वानों में से एक थे। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले उनका नाम एंसेलम टोरमेडा था। जब ईश्वर ने उनका हृदय खोला और उन्हें इस्लाम की ओर निर्देशित किया, तो उन्होंने स्वयं को अब्दुल्ला कहा, और उनके साथ तरजुमान की उपाधि जुड़ गई क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने ट्यूनिस के सुल्तान के लिए अनुवादक के रूप में काम किया। उन्होंने 823 हिजरी में अरबी में "तुहफत अल-अरीब फी अल-रद्द अला अहल अल-सलिब" नामक पुस्तक लिखी, जिसका बाद में फ्रेंच में अनुवाद किया गया और 1885 ई. में पेरिस की "धर्मों का इतिहास" पत्रिका में प्रकाशित किया गया।
अब्दुल्ला अल-तरजुमान के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
अब्दुल्ला अल-तर्जुमन ने अपनी पुस्तक तुहफत अल-अरीब में इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी सुनाई: जान लो, ईश्वर तुम पर दया करे, कि मैं मूल रूप से मालोर्का शहर से हूँ। मेरे पिता को वहाँ के लोगों में से एक माना जाता था, और मेरे अलावा उनकी कोई और संतान नहीं थी। जब मैं छह साल का था, तो उन्होंने मुझे एक पादरी शिक्षक को सौंप दिया। मैंने उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाई, जब तक कि दो साल में मुझे आधी से ज़्यादा याद नहीं हो गई। फिर मैंने छह साल में बाइबल की भाषा और तर्कशास्त्र सीखना शुरू किया। फिर मैं मालोर्का शहर से कैटेलोनिया के लेइडा शहर गया, जो उस देश के ईसाइयों के बीच ज्ञान का शहर है। इस शहर में ज्ञान के ईसाई छात्र इकट्ठा होते हैं। मैंने छह साल तक प्राकृतिक विज्ञान और तारों का अध्ययन किया, और फिर मैंने चार साल तक बाइबल पढ़ना और उसे पढ़ाना शुरू किया।
फिर मैं बोलोग्ना शहर गया और वहीं बस गया। यह ज्ञान का शहर है और इसमें निकोले मार्टेल नामक एक बुज़ुर्ग और प्रतिष्ठित पादरी का चर्च है। ज्ञान, धर्म और तप में उनका स्थान बहुत ऊँचा था। ईसाई धर्म और दान के बारे में प्रश्न राजाओं और अन्य लोगों से उनके पास आते थे। वे उनसे आशीर्वाद पाने और उनके दान स्वीकार करने और उससे सम्मानित होने की भी इच्छा रखते थे। इसलिए मैंने इस पादरी को ईसाई धर्म के सिद्धांत और उसके नियम पढ़कर सुनाए और उनकी सेवा और उनके कई कर्तव्यों का पालन करके मैं उनके करीब आता रहा, जब तक कि उन्होंने मुझे अपना सबसे अच्छा विश्वासपात्र नहीं बना लिया और मुझे अपने निवास और खाने-पीने के भंडार की चाबियाँ नहीं दे दीं। मैं दस साल तक उनके साथ रहकर उन्हें पढ़कर सुनाता रहा और उनकी सेवा करता रहा। फिर एक दिन वे बीमार पड़ गए और अपने पाठ सत्र में अनुपस्थित रहे। सभा में उपस्थित लोग ज्ञान की बातों पर चर्चा करते हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे, जब तक कि बातचीत उन्हें अपने नबी ईसा (उन पर शांति हो) की ज़ुबान पर सर्वशक्तिमान ईश्वर के इन शब्दों तक नहीं ले गई: "मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम पराक्लीट है।" उन्होंने चर्चा की कि यह नबी नबियों में से कौन है और उनमें से हर एक ने अपने ज्ञान और समझ के अनुसार बात की। इस बारे में उनके बीच बहुत बहस हुई और उनका तर्क-वितर्क बढ़ गया, फिर वे उस मामले में रुचि लेने के बिना ही चले गए।
इसलिए मैं उस शेख के घर गया जिसने ऊपर बताया गया पाठ पढ़ाया था। उसने मुझसे कहा, "आज जब मैं तुमसे दूर था, तब तुमने क्या चर्चा की?" मैंने उसे पैराक्लीट के नाम पर लोगों की असहमति के बारे में बताया और बताया कि फलां ने फलां से ऐसा और फलां ने फलां से ऐसा उत्तर दिया था। मैंने उन्हें उनके उत्तर सुनाए, और उसने मुझसे पूछा, "और तुमने क्या उत्तर दिया?" मैंने कहा, "न्यायाधीश फलां ने सुसमाचार की अपनी व्याख्या में जो उत्तर दिया था।" उसने मुझसे कहा, "तुम चूके नहीं, बल्कि करीब पहुँच गए। फलां ने गलती की, और फलां लगभग करीब पहुँच गए थे। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि इस महान नाम की व्याख्या केवल वे विद्वान ही जानते हैं जो ज्ञान में दृढ़ हैं, और तुमने तो बहुत कम ज्ञान अर्जित किया है।"
इसलिए मैंने जल्दी से उनके पैर चूमे और उनसे कहा, "मेरे स्वामी, आप जानते हैं कि मैं एक दूर देश से आपके पास आया हूँ और दस वर्षों से आपकी सेवा में हूँ, इस दौरान मैंने आपसे इतना ज्ञान अर्जित किया है जिसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। शायद यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस महान नाम का ज्ञान दिया है।" वृद्ध व्यक्ति रो पड़ा और बोला, "बेटा, ईश्वर की शपथ, तुम मेरी सेवा और मेरे प्रति अपनी भक्ति के कारण मुझे बहुत प्रिय हो। इस महान नाम को जानने में बहुत लाभ है, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई, तो ईसाई तुम्हें तुरंत मार डालेंगे।"
तो मैंने उससे कहा: ऐ मेरे मालिक, सर्वशक्तिमान ईश्वर और इंजील की सच्चाई और उसके लाने वाले की कसम, मैं आपकी आज्ञा के बिना आपके द्वारा बताई गई किसी भी बात के बारे में बात नहीं करूँगा। उसने मुझसे कहा: ऐ मेरे बेटे, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तो मैंने तुमसे तुम्हारे देश के बारे में पूछा था और यह भी कि क्या यह मुसलमानों के करीब है और क्या वे तुम्हें स्वीकार करते हैं या तुम उन्हें स्वीकार करते हो, ताकि इस्लाम के प्रति तुम्हारे विरोध को परख सको। जान लो, मेरे बेटे, कि पराक्लीट उनके पैगंबर मुहम्मद के नामों में से एक है, और इसके आधार पर, उपरोक्त चौथी किताब दानिय्येल (उन पर शांति हो) की ज़ुबान से उतरी थी, और उन्होंने मुझे सूचित किया कि यह किताब उन पर अवतरित होगी और उनका धर्म सत्य का धर्म है और उनका पंथ इंजील में वर्णित श्वेत पंथ है।
मैंने कहा: ऐ मेरे आका, इन ईसाइयों के धर्म के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने मुझसे कहा: ऐ मेरे बेटे, अगर ईसाई पहले ईसा के धर्म पर चलते, तो वे ईश्वर के धर्म पर होते, क्योंकि ईसा और सभी पैगम्बरों का धर्म ईश्वर का धर्म था। मैंने कहा: ऐ मेरे आका, हम इस मामले से कैसे बच सकते हैं? उन्होंने कहा: ऐ मेरे बेटे, इस्लाम धर्म में प्रवेश करके। मैंने उनसे कहा: क्या इसमें प्रवेश करने वाला बच जाएगा? उन्होंने मुझसे कहा: हाँ, वह इस दुनिया और परलोक में बच जाएगा।
मैंने उनसे कहा: हे मेरे स्वामी, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए केवल वही चुनता है जो वह जानता है। इसलिए यदि आप इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को जानते हैं, तो आपको इससे क्या रोकता है? उन्होंने मुझसे कहा: हे मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता और इस्लाम धर्म के सम्मान के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया था, उसकी सच्चाई से तब तक अवगत नहीं कराया जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो गया और मेरी हड्डियाँ कमजोर नहीं हो गईं। हमारे पास इसके लिए कोई बहाना नहीं है; बल्कि, अल्लाह का प्रमाण हमारे खिलाफ स्थापित है। यदि अल्लाह ने मुझे आपकी उम्र में इसका मार्गदर्शन किया होता, तो मैं सब कुछ त्याग कर सत्य को अपना लेता। इस दुनिया का प्रेम हर पाप की जड़ है। आप देख रहे हैं कि मैं ईसाइयों के बीच उच्च पद, सम्मान, गौरव और सांसारिक अवसरों की प्रचुरता के मामले में कैसा हूँ। अगर इस्लाम धर्म के प्रति मुझमें थोड़ा सा भी झुकाव दिखाई देता, तो आम लोग मुझे तुरंत मार डालते।
यदि मैं उनसे बचकर मुसलमानों के पास पहुँच भी जाऊँ और उनसे कह दूँ कि मैं मुसलमान होकर आपके पास आया हूँ, और वे मुझसे कहें कि, "सत्य के धर्म में प्रवेश करके तुमने स्वयं को लाभ पहुँचाया है, अतः हमें उस धर्म का बखान मत करो जिसके द्वारा तुमने स्वयं को ईश्वर की यातना से बचाया है," तो मैं उनके बीच नब्बे वर्ष का एक बूढ़ा, दरिद्र व्यक्ति रहूँगा, उनकी भाषा नहीं समझूँगा और वे मेरा अधिकार नहीं जानेंगे, और मैं उनके बीच भूख से मर जाऊँगा।
और मैं, ईश्वर की स्तुति हो, ईसा के धर्म और उनके द्वारा लाए गए धर्म का पालन कर रहा हूँ, और ईश्वर मेरे विषय में यह जानता है। इसलिए मैंने उनसे कहा: हे मेरे स्वामी, क्या आप मुझे मुसलमानों की भूमि पर चलने और उनके धर्म में प्रवेश करने की अनुमति देंगे? उन्होंने मुझसे कहा: यदि आप मोक्ष चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो ऐसा करने में जल्दी करो, और आप इस दुनिया और उसके बाद को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे बेटे, यह एक ऐसा मामला है कि अब हमारे साथ कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए जितना हो सके इसे गुप्त रखो, और यदि इसके बारे में कुछ भी पता चला, तो लोग तुम्हें तुरंत मार देंगे, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। इसे मुझसे प्रसारित करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका खंडन करता हूँ, और आपके बारे में मेरा कथन सत्य है, और मेरे बारे में आपका कथन सत्य नहीं है, और यदि आप इसके बारे में कुछ भी कहते हैं तो मैं आपके खून से निर्दोष हूँ।
मैंने कहा: हे मेरे स्वामी, मैं इस भ्रम के फैलने से ईश्वर की शरण में आता हूँ, और मैंने उनसे वादा किया कि जो उन्हें प्रसन्न करेगा, फिर मैंने यात्रा का साधन लिया और उन्हें विदा किया, तो उन्होंने मेरी भलाई के लिए प्रार्थना की और मुझे पचास स्वर्ण दीनार प्रदान किए, और मैं समुद्र पर सवार होकर मालोर्का शहर की ओर चल पड़ा, और मैं वहाँ छह महीने तक रहा, फिर मैं वहाँ से सिसिली शहर गया, और मैं वहाँ पाँच महीने तक रहा, जब तक कि मैं मुसलमानों की भूमि पर जाने के लिए एक जहाज की प्रतीक्षा करता रहा, और एक जहाज ट्यूनिस शहर की यात्रा करने के लिए आया, इसलिए मैंने सिसिली से उसमें यात्रा की, और हम सूर्यास्त के निकट रवाना हुए, और हम दोपहर के करीब ट्यूनिस के बंदरगाह पर पहुँचे।
जब मैं ट्यूनिस के दीवान पहुँचा और वहाँ के ईसाई रब्बियों ने मेरे बारे में सुना, तो वे एक घोड़ा लेकर आए और मुझे अपने साथ अपने देश ले गए। मैं उनके साथ चार महीने तक बेहद आरामदायक माहौल में उनके मेहमान की तरह रहा। उसके बाद, मैंने उनसे पूछा कि क्या सल्तनत में कोई ऐसा है जो ईसाइयों की भाषा में पारंगत हो। उस समय सुल्तान हमारे स्वामी अबू अल-अब्बास अहमद थे, ईश्वर उन पर दया करे। ईसाइयों ने मुझे बताया कि सल्तनत में एक नेक इंसान रहता है, जो उनके सबसे बड़े सेवकों में से एक था, जिसका नाम यूसुफ़ हकीम था, जो उनका हकीम और उनका एक विश्वासपात्र था। मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ, और मैंने उस हकीम के निवास के बारे में पूछा, और मुझे उसके पास भेजा गया और मैं उससे मिला। मैंने उसे अपनी हालत और अपने आने का कारण, यानी इस्लाम धर्म अपनाने के बारे में बताया। वह व्यक्ति इससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह नेकी उसी के हाथों पूरी हुई थी।
फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर मुझे अपने साथ सुल्तान के महल में ले गया। उसने अंदर जाकर उसे मेरी कहानी सुनाई और मुझसे मिलने की इजाज़त माँगी, तो उसने मुझे इजाज़त दे दी। मैं उसके सामने खड़ा था और सबसे पहले उसने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तो मैंने उसे बताया कि मैं पैंतीस साल का हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैंने विज्ञान के बारे में क्या पढ़ा है, तो मैंने उसे बताया। उसने कहा: मैं सौभाग्य से आया हूँ और अल्लाह तआला की कृपा से मुसलमान बन गया हूँ। मैंने दुभाषिए से, जो ऊपर वर्णित चिकित्सक था, कहा: हमारे स्वामी सुल्तान से कहो कि कोई भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, सिवाय इसके कि उसका परिवार उसके बारे में बहुत कुछ बोले और उसकी आलोचना करे। इसलिए मैं आपकी दया से चाहता हूँ कि आप उन ईसाई व्यापारियों और उनके अच्छे लोगों को भेजें जो आपके साथ हैं और उनसे मेरे बारे में पूछें और सुनें कि वे मेरे बारे में क्या कहते हैं, और फिर मैं मुसलमान बन जाऊँगा, अल्लाह की इच्छा से। उसने दुभाषिए के माध्यम से मुझसे कहा: आपने वही पूछा जो अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने पैगंबर से पूछा था, अल्लाह उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे, और फिर वह मुसलमान बन गए।
इसलिए उसने सबसे अच्छे ईसाइयों और उनके कुछ व्यापारियों को बुलाया और मुझे अपने बैठक कक्ष के पास एक घर में ले गया। जब ईसाई उसके पास आए, तो उसने उनसे कहा, "इस जहाज में आए इस नए पादरी के बारे में तुम क्या कहते हो?" उन्होंने कहा, "महाराज, यह हमारे धर्म का एक महान विद्वान है, और हमने ज्ञान और धर्म में उससे ऊँचा कोई नहीं देखा।" उसने उनसे कहा, "और अगर वह मुसलमान बन जाए, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे?" उन्होंने कहा, "हम इससे बचने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं; वह ऐसा कभी नहीं करेगा।" जब उसने ईसाइयों की बातें सुनीं, तो उसने मुझे बुलाया, और मैं उसके सामने उपस्थित हुआ और ईसाइयों की उपस्थिति में सच्चाई की गवाही दी। वे मुँह के बल गिर पड़े और बोले, "विवाह के प्रेम के अलावा किसी और चीज़ ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया है, क्योंकि हमारे पादरी विवाह नहीं करते।" इसलिए वे व्यथित और उदास होकर चले गए।
सुल्तान, अल्लाह उन पर रहम करे, मेरे लिए रोज़ाना एक चौथाई दीनार का इंतज़ाम करते थे। जब मैंने शादी करने का फ़ैसला किया, तो उन्होंने मुझे सोने के सौ दीनार और एक पूरा, अच्छा कपड़ा दिया। मैंने अपनी पत्नी से शादी की और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने हमारे पैगम्बर मुहम्मद के आशीर्वाद से मुहम्मद रखा, अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे।[1]
फातिमा हिरिन
इस्लाम का सच्चा अर्थ यह है कि विश्वासियों को अपने आप में तथा अपने छोटे-बड़े मामलों में सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए।
विश्वास, आश्वस्त और संतुष्ट आज्ञाकारिता के साथ उस हाथ के आगे समर्पण करना जो उन्हें मार्गदर्शित करता है, जबकि यह निश्चित है कि वह उनके लिए भलाई, सलाह और मार्गदर्शन चाहता है, और इस दुनिया और परलोक में समान रूप से मार्ग और भाग्य के बारे में आश्वस्त है; सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों के अनुसार: {कहो, "निश्चय ही मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानी और मेरा जीवन और मेरी मृत्यु अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है। * उसका कोई साझी नहीं है। और मुझे इसका आदेश दिया गया है, और मैं पहला मुसलमान हूँ।"} [अल-अनआम: 162-163]
यह वह मुद्दा था जिसने जर्मन लड़की फातिमा हीरेन को चिंतित कर दिया था, जिसने राष्ट्रीय समाजवाद की शिक्षाओं के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिसमें ईश्वर की भूमिका सृष्टि के हर पहलू या लोगों के दैनिक जीवन से गायब हो जाती है।
राष्ट्रवादी नारे
फातिमा हेरेन का जन्म 1934 में जर्मनी में हुआ था। उनके पिता जर्मन सेना में कार्यरत थे और राष्ट्रीय समाजवादी मूल्यों को महत्व देते थे।
1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब फ़ातिमा ग्यारह साल की छात्रा थीं। जर्मन राष्ट्र के सपने चकनाचूर हो चुके थे, और वे सभी आदर्श, जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तिरोहित हो चुके थे।
युद्ध से पहले और उसके दौरान के वर्षों में राष्ट्रवाद जर्मनों को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक उत्कृष्ट साधन था, जिसमें उनकी एकमात्र चिंता मातृभूमि के लिए सब कुछ करने की थी।
इस राष्ट्रवाद का ईश्वर के अस्तित्व के विचार पर भी प्रभाव पड़ा। जर्मन समाज के लिए, ईश्वर वह शक्ति थी जिसने लाखों साल पहले प्रकृति के नियमों की स्थापना की थी, और इन्हीं नियमों ने, संभवतः संयोगवश, मानव का निर्माण किया था।
फातिमा हिरीन उस समय अपने समाज की वैचारिक स्थिति के बारे में कहती हैं: "ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म था जो वास्तव में हमारे सामने था, और इसे हमारे सामने 'लोगों की अफीम' के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और भेड़ों के झुंड के धर्म के रूप में जो केवल मृत्यु के भय से चलता है।
हमने समझा कि हर व्यक्ति अपने लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार है, और वह अपने साथ जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते इससे दूसरों को कोई नुकसान न हो। हमने सोचा कि विवेक ही एकमात्र ऐसा प्रकाशस्तंभ है जो हमारा मार्गदर्शन करता है।
"मेरे जैसे कई लोग आधुनिक समाज की स्थिति से खुश नहीं थे; लेकिन वे खुश होने का दावा करते थे, और जब वे नाचने और नशे में धुत्त रहने के बाद रात को उठते थे, तो उन्हें अपने सीने में एक खालीपन महसूस होता था, और अगली शाम को और अधिक नाचने, शराब पीने या छेड़खानी करके खुद को सांत्वना देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था।"
जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो फातिमा ने कहा: "युद्ध ने न केवल हमारे देश (जर्मनी) को तोड़ दिया, बल्कि हमारे राष्ट्र की महानता को भी चकनाचूर कर दिया, और वे सभी आदर्श नष्ट हो गए जिनके लिए जीवन का बलिदान दिया गया था।
मुझे एहसास हुआ कि व्यक्तिगत विवेक और समाज में मान्यता प्राप्त मानवीय आदर्श ही मेरे जीवन में मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मुझे उपलब्ध सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हुए, मुझे उन सभी अच्छाइयों के लिए किसी का धन्यवाद किए बिना सच्ची खुशी का अनुभव नहीं होता था जो मुझे घेरे हुए थीं। इसलिए मैंने अपनी दैनिक डायरी लिखने के लिए एक नोटबुक रखी, और एक बार मैंने खुद को उसमें निम्नलिखित वाक्यांश लिखते हुए पाया: "यह एक आनंदमय दिन था; बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रभु!"
पहले तो मुझे शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सिर्फ़ ईश्वर पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है... जब तक मुझे यह पता नहीं चला कि उसे खोजने के लिए काम करना, और उसे धन्यवाद देने और उसकी आराधना करने का तरीक़ा ढूँढ़ना मेरा कर्तव्य है।”
ईसाई धर्म की अमान्यता
अपने देश की राष्ट्रीय परियोजना सभ्यता और आस्था के मामले में विफल होने के बाद, फ़ातिमा हिरिन ने ईश्वर तक पहुँचने की आशा में ईसाई धर्म अपना लिया। फ़ातिमा कहती हैं: "मैंने एक पादरी से शिक्षा ली, कुछ ईसाई पुस्तकें पढ़ीं और चर्च की प्रार्थना सभाओं में भाग लिया, लेकिन मैं ईश्वर के करीब नहीं पहुँच सकी। एक पादरी ने मुझे ईसाई धर्म अपनाने और प्रभु भोज में जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा: 'क्योंकि जब आप ईसाई धर्म का पालन करेंगे, तो आपको ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता ज़रूर मिलेगा।' मैंने उनकी सलाह मानी, लेकिन मुझे सच्ची मानसिक शांति नहीं मिली।"
फ़ातिमा हिरेन ने बताया कि ईसाई धर्म में उनकी निराशा का कारण यह है कि हम ईसाइयों के पास अपने समाज में जीने के लिए अपनी आस्था में रियायतें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चर्च हमारे समाज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हमेशा समझौते करने को तैयार रहता है। एक उदाहरण देते हैं: चर्च कहता है कि ईश्वर के नाम पर विवाह से पहले यौन संबंध शुरू नहीं करने चाहिए, लेकिन पश्चिम में लगभग कोई भी पुरुष या महिला "झूठी बात" को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह एक आम कहावत है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति दोनों साथियों की यौन अनुकूलता की जाँच किए बिना ही विवाहित जीवन में प्रवेश कर जाता है।
पुजारी हमेशा एक या दो प्रार्थना करके इस पाप को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं!!”
उपरोक्त के विपरीत, इस्लाम अपने अनुयायियों से, आस्था के नाम पर, बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का आह्वान करता है। इस समर्पण से असंगत विचारों या भावनाओं, इरादों या कार्यों, इच्छाओं या भय का कोई अवशेष नहीं बचता जो ईश्वर के प्रति समर्पण न करें या उसके निर्णय और आदेश को स्वीकार न करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं: {ऐ ईमान वालों, पूरी तरह से इस्लाम में प्रवेश करो और शैतान के नक्शेकदम पर मत चलो। निस्संदेह, वह तुम्हारा स्पष्ट शत्रु है।} [अल-बक़रा: 208]
फ़ातिमा हिरीन और इस्लाम का मार्ग
फातिमा हिरीन एक पूर्ण सिद्धांत पर विश्वास करने की आशा कर रही थी, एक सीधा मार्ग जिस पर वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगी; इसलिए, वह चर्च में घुटने टेकते हुए भी परमेश्वर के पास जाने में असमर्थ थी।
1957 में, फ़ातिमा हेरिन की पहली मुलाक़ात उस व्यक्ति से हुई जो दो साल बाद उनका पति बनने वाला था। वह एक जर्मन मुसलमान था जिसने दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी।
फ़ातिमा उनके बारे में कहती हैं: "वह एक साधारण इंसान थे, किसी भी दूसरे जर्मन व्यक्ति से अलग नहीं। हालाँकि, जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सात साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था, तो मैं बहुत हैरान हुई। मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता जागी कि इतने पढ़े-लिखे इंसान ने यह रास्ता क्यों चुना।"
मेरे पति मुझे इस्लाम का अर्थ समझाने लगे। उन्होंने कहा: ईश्वर केवल मुसलमानों का ही प्रभु नहीं है, बल्कि यह शब्द "ईश्वर" हमारे लिए "ईश्वरत्व" का पर्याय है। मुसलमान सृष्टिकर्ता की पूर्ण एकता में विश्वास करते हैं, और वे अपने पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति और आशीर्वाद हो) की पूजा नहीं करते, जैसा कि ईसाई ईसा मसीह (उन पर शांति हो) की पूजा करते हैं। "इस्लाम" शब्द का अर्थ है एकमात्र ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण।
उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामी दृष्टिकोण से सभी प्राणी और सभी चीजें अनिवार्यतः मुसलमान हैं; अर्थात्, उन्हें ईश्वर के नियमों के प्रति समर्पित होना चाहिए, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके विलुप्त होने का खतरा है।
उन्होंने आगे कहा: "मनुष्य को, चाहे वह स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम धर्म अपनाए, ईश्वर ने अपनी इच्छा और चुनाव की स्वतंत्रता दी है कि वह अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में मुसलमान बनना चाहता है या नहीं। यदि वह ऐसा करता है और इस निर्णय के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो वह ईश्वर से जुड़ जाएगा और इस सांसारिक जीवन में अन्य प्राणियों के साथ सामंजस्य और मन की शांति प्राप्त करेगा, और उसे परलोक में भी सुख मिलेगा।"
लेकिन अगर वह ईश्वर के नियमों के खिलाफ विद्रोह करता है, जो पवित्र कुरान में स्पष्ट और शानदार ढंग से हमारे लिए समझाया गया है, तो वह इस सांसारिक जीवन और उसके बाद में घाटे में है। ”
फ़ातिमा इस्लाम के बारे में अपनी खोज के बारे में आगे कहती हैं: "मैंने अपने पति से यह भी सीखा कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। दरअसल, क़ुरान ही एकमात्र ऐसी किताब है जो किसी भी तरह की अशुद्धता या ग़लती से मुक्त है। यह किताबों की एक लंबी श्रृंखला की आखिरी ईश्वरीय किताब है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं तौरात और बाइबल में दिए गए इलहाम।
इस तरह, एक नई दुनिया की संभावनाएँ मेरी आँखों के सामने खुल गईं। अपने पति के मार्गदर्शन में, मैंने जर्मन में इस्लाम पर उपलब्ध कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया, और मेरा मतलब इस्लामी दृष्टिकोण से उपलब्ध कुछ किताबों से है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुहम्मद असद की किताब (मक्का की राह) थी, जो मेरे लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी।
हमारी शादी के कुछ महीनों बाद, मैंने अरबी में प्रार्थना करना, रोज़ा रखना और पवित्र कुरान का अध्ययन करना सीखा, और यह सब मैंने 1960 में इस्लाम धर्म अपनाने से पहले किया।
क़ुरआन की बुद्धिमत्ता ने मेरी आत्मा को प्रेम और प्रशंसा से भर दिया, लेकिन मेरी आँखों का आनंद प्रार्थना में था। मुझे एक प्रबल अनुभूति हुई कि जब मैं ईश्वर के सामने विनम्रतापूर्वक खड़ा होकर क़ुरआन पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो ईश्वर मेरे साथ थे।
इस्लाम एक जीवन शैली है
फातिमा हिरीन ने धर्म को अपने जीवन का एक सीमित हिस्सा ही रहने देने से इनकार कर दिया, जैसा कि पहले था, या शायद धर्म को कभी कोई हिस्सा ही नहीं मिला था।
फातिमा ने जीवन भर इस्लाम के अनुसार जीने का निर्णय लिया और इसे अपने जीवन का सम्पूर्ण दृष्टिकोण बनाने का निर्णय लिया, भले ही इसके लिए उन्हें देश से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा।
फातिमा हिरीन कहती हैं: “मैंने नियमित रूप से पाँचों नमाज़ें अदा करना शुरू कर दिया, और मैंने सीखा कि नमाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बेतरतीब ढंग से किया जा सके, बल्कि यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसका पूरे दिन पालन किया जाना चाहिए।
मैंने इस्लामी हिजाब पहनने का फैसला किया, और मैंने उस स्थिति को स्वीकार करना सीख लिया जहाँ मेरे पति अपने धार्मिक भाइयों के साथ बैठते, उनके साथ ज्ञानवर्धक बातें करते, जबकि मैं उनके लिए चाय बनाती और दरवाज़े पर परोसती, उन लोगों को बताए बिना जिनके लिए मैंने चाय बनाई थी। बाज़ार जाने के बजाय, मुझे घर पर रहकर अंग्रेज़ी में इस्लामी किताबें पढ़ने की आदत हो गई।
मैंने उपवास भी शुरू कर दिया था, और कई बार बहुत भूख और प्यास लगने के बावजूद मैं बिना चखे ही भोजन तैयार कर लेती थी।
मैंने पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति और आशीर्वाद हो) और उनके साथियों से महान पैगंबरी हदीसों की किताबें पढ़कर प्रेम करना सीखा। मेरी नज़र में, वे सिर्फ़ अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण नहीं, बल्कि जीवित मानव आकृतियाँ बन गए।
इन प्रारंभिक लोगों ने अपने मानव जीवन में जो करुणा, साहस, भक्ति और धार्मिकता के उदाहरण स्थापित किए, वे मेरे लिए मार्गदर्शक बन गए, और मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार आकार दूं जिससे मैं इस सांसारिक जीवन में अच्छे और संतुष्ट लोगों में से एक बन सकूं, और यही वह मार्ग है जिस पर हमारा आचरण यह निर्धारित करता है कि हमें परलोक में किस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा।”
फ़ातिमा हिरीन इस्लाम के अनुसार जीने और उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं पर लागू करने का प्रयास करती हैं, और कहती हैं, "मेरे पति और मैं इस बात पर सहमत थे कि एक पश्चिमी देश में हमारी इस्लामी जीवनशैली के लिए हमें कई रियायतें देनी पड़ती हैं। इस्लाम केवल एक सामान्य धर्म नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जिसे केवल एक मुस्लिम समाज में ही अपने शुद्धतम रूप में लागू किया जा सकता है। चूँकि हम सभी ने पूरी स्वतंत्र इच्छा से इस धर्म को चुना था, इसलिए हम एक कमज़ोर, गुनगुना इस्लाम नहीं चाहते थे।"
इसलिए, लंबे इंतजार के बाद, हमें 1962 में पाकिस्तान में प्रवास करने का अवसर मिला, क्योंकि हमने यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया था।”
फ़ातिमा हिरीन और इस्लाम की रक्षा
फ़ातिमा ने इस्लाम का बचाव किया और इस्लामी क़ानून की महानता और पवित्रता का प्रदर्शन किया, साथ ही अन्य मान्यताओं के झूठ और गुमराही को भी उजागर किया। उन्होंने कहा: "अगर इस्लाम के विरोधी कहते हैं कि एक पुरुष का कई पत्नियाँ रखना बर्बरता है, तो क्या वे मुझे बता सकते हैं कि जब एक पति अपनी पत्नी के अलावा रखैलें रखता है, तो उनके इस कृत्य में क्या अच्छाई है? यह पश्चिम में एक आम प्रथा है, जो मुस्लिम देशों में बहुविवाह से भी ज़्यादा प्रचलित है।"
यदि वे दावा करते हैं कि शराब पीने से उन्हें कोई नुकसान नहीं है, तो क्या वे पश्चिम में इस आदत के कारण होने वाले दुख की व्याख्या कर सकते हैं?
यदि वे कहते हैं कि उपवास से राष्ट्र की कार्यबल और स्वास्थ्य कमजोर होता है, तो उन्हें रमजान के पवित्र महीने के दौरान विश्वासियों की महान उपलब्धियों पर गौर करना चाहिए, तथा हाल ही में मुस्लिम डॉक्टरों द्वारा उपवास करने वाले रोगियों के साथ उनके प्राकृतिक अनुभवों के बारे में दर्ज की गई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए।
अगर वे कहते हैं कि लिंग भेद करना पिछड़ापन है, तो उन्हें किसी भी मुस्लिम देश के युवाओं की तुलना किसी भी पश्चिमी देश के युवाओं से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मुसलमानों में लड़के और लड़की के बीच नैतिक अपराध को अपवाद माना जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में एक भी पवित्र लड़के और लड़की के बीच विवाह होना बहुत दुर्लभ है।
अगर इस्लाम के विरोधी यह दावा करते हैं कि पाँचों वक़्त की नमाज़ें—ऐसी भाषा में जो कई धर्मावलंबियों को नहीं पता—करना समय और मेहनत की बर्बादी है, तो उन्हें पश्चिम में एक ऐसी व्यवस्था बतानी चाहिए जो लोगों को मुस्लिम रीति-रिवाज़ों की तुलना में ज़्यादा मज़बूत और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ तरीके से एकजुट करती हो। उन्हें यह साबित करना चाहिए कि पश्चिमी लोग अपने खाली समय में उस मुसलमान से ज़्यादा उपयोगी काम करते हैं जो रोज़ाना एक घंटा नमाज़ के लिए निकालता है।
इस्लाम में चौदह शताब्दियों या उससे अधिक समय से सुधार हो रहा है, और यह हमारे समय में भी बना हुआ है, बशर्ते हम इसे विकृत रियायतों के बिना आगे बढ़ाएं।
क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में धर्म इस्लाम है, और इस्लाम सर्वोच्च है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारे समय में बहुत से लोग इस सत्य के प्रति आश्वस्त हो गए हैं, और वे - ईश्वर की इच्छा से - उस बीमार, पीड़ित और दुखी दुनिया को, जो उनका सम्मान करती है, इसे समझाने में सहयोग करेंगे।”
इस्लाम धर्म अपनाने के बाद फ़ातिमा हिरीन की ज़िंदगी इस तरह बदल गई। उनका मानना था कि इस्लाम सिर्फ़ रस्में और इबादत नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति और एक ऐसा रास्ता है जो मुसलमानों को इस दुनिया में खुशी और परलोक में जन्नत की ओर ले जाता है।
फ़ातिमा हिरीन का योगदान
इस्लाम पर उनकी कई किताबें हैं, जिनमें शामिल हैं: (उपवास - दास फास्टन) 1982, (ज़कात - ज़कात) 1978, और (मुहम्मद - मुहम्मद) 1983।
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
लुई जार्डेट
लुई गार्डेट को उन सबसे प्रमुख यूरोपीय दार्शनिकों में से एक माना जाता है जिन्होंने इस्लामी विचार और सभ्यता का सचेत और गहन अध्ययन किया है। छोटी उम्र से ही, गार्डेट ईश्वरीय धर्मों के सिद्धांतों को समझने के लिए उत्सुक थे। हालाँकि उनका पालन-पोषण एक रूढ़िवादी कैथोलिक परिवार में हुआ था, फिर भी वे एक मनोवैज्ञानिक जुनून से ग्रस्त थे: अपने ही धर्म में छिपे रहस्यों और रहस्यों से। इसी जुनून ने उन्हें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य पूर्वी धर्मों की उत्पत्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया, ताकि सत्य को उजागर किया जा सके।
लुई जार्डेट के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
ईश्वर की इच्छा थी कि लुई गार्डेट कुरान के अर्थों का अपना अनुवाद पढ़ें, और उन्होंने उसमें कई ऐसी बातें पाईं जिनसे उनके हृदय को शांति मिली। वे इस्लाम की ओर आकर्षित हुए और धीरे-धीरे इस्लाम में गहराई से उतरने लगे। उन्होंने अरबी सीखी और अरबी में कुरान पढ़ा। फिर उन्होंने इस्लामी सभ्यता का अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि इस्लाम ही वह चीज़ है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे इसे एक सच्चे ईश्वरीय विश्वास के रूप में मानते थे (अपने हृदय में), क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो लोग इस्लाम अपनाते हैं और यूरोप में इसका प्रचार करते हैं, उन्हें आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, गार्डेट ने अपने विश्वास को अपने भीतर ही छिपा लिया और अपने प्रयासों, काम, धन और विचारों को इस धर्म के समर्थन तक सीमित कर दिया।
लुई गार्डेट ने कहा कि ज़ायोनिज़्म यूरोप में इस्लामी हर चीज़ के विरुद्ध एक आक्रामक युद्ध छेड़ रहा है, सभी प्रकार के आक्रामक तरीकों का उपयोग कर रहा है, जिसकी शुरुआत पवित्र कुरान की कुछ आयतों को विकृत करने के प्रयासों से होती है, पवित्र कुरान को विकृत करने के बाद इसे कई अफ्रीकी क्षेत्रों में निर्यात करना, इस्लामी पैटर्न और प्रतीकों के साथ अंडरवियर और जूते डिजाइन करना जो हर मुसलमान के विवेक में पवित्र और सम्मानित हैं, और कट्टरपंथी शोधकर्ताओं को अपनी किताबें और अध्ययन प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने में योगदान देना जो इस्लाम की छवि को विकृत करते हैं और मुसलमानों और उनके पैगम्बर पर दोष और बुराइयाँ आरोपित करते हैं।
लुई गार्डेट का योगदान
लुई गार्डेट ने इस्लाम का बचाव किया और "मुस्लिम और ज़ायोनी हमलों का सामना" नामक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने टूलूज़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय दर्शनशास्त्र संस्थान में पूरे पंद्रह वर्षों (1957-1972 ई.) तक इस्लामी दर्शन का अध्ययन भी किया।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण इस्लामी कृतियों की भी रचना की है, जैसे: इस्लामिक सोसाइटी, इस्लाम फॉर ऑल एजेस, और रिलिजन एंड सोसाइटी। वे इस्लामी अध्ययनों की एक श्रृंखला के प्रकाशन का पर्यवेक्षण करते हैं और फ्रेंच में इस्लामिक विश्वकोश के विकास में भी योगदान देते हैं।
उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक पुस्तक (इस्लाम सभी युगों के लिए एक धर्म है) है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इस्लामी मूल्य और सिद्धांत सभी युगों और पीढ़ियों में बने रहने में सक्षम रहे हैं, और हर युग में नए, नवीनीकृत, मांग में और प्रभावशाली बने रहे हैं !!
इस पुस्तक में, गार्डेट कुछ दार्शनिक सिद्धांतकारों के इस दावे को भी खारिज करते हैं कि इस्लाम एक "रेगिस्तानी धर्म" है और अन्य समाजों के साथ असंगत है। वे इन भौतिकवादियों को यह कहते हुए जवाब देते हैं: "जब यह नया धर्म आया, तो रेगिस्तान केवल उसका स्थान और प्रस्थान बिंदु था। वहाँ इसकी नींव पक्की हुई और इसकी विशेषताएँ स्पष्ट हुईं, क्योंकि यह एक वैश्विक धर्म बन गया। रेगिस्तान किसी भी तरह से इस्लामी लोगों के लिए एक स्थिर स्थान नहीं था, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि आज इस्लामी दुनिया में एक अरब से ज़्यादा मुसलमान शामिल हैं, और यह सेनेगल के डकार से लेकर हिंद महासागर में स्थित फ़िलिपीनी द्वीप समूह तक फैला हुआ है।"
लुई गार्डेट और इस्लाम की रक्षा
जार्डेट पश्चिमी देशों द्वारा इस्लाम और मुसलमानों के बारे में की गई, प्रचारित और दोहराई गई बदनामी का जवाब देते हैं, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि मुसलमान "भाग्यवादी और आश्रित" हैं। वह दर्जनों कुरान की आयतों और हदीसों के ज़रिए मुसलमानों से कड़ी मेहनत करने और अपना काम अच्छी तरह से करने और पूरी ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह करते हैं। इसके बाद वह इस आरोप का जवाब देते हैं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दिखावटी रीति-रिवाजों और समारोहों का है, जो रोज़मर्रा के व्यवहार की परवाह किए बिना किए जाते हैं। वह निम्नलिखित प्रतिक्रिया देते हैं:
"ऐसी बातें पतन के युग में सामने आईं, और सच्चाई यह है कि जब तक पूजा सच्ची और शुद्ध इरादों से न की जाए, तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।"
इस्लाम के बारे में पश्चिमी लोगों द्वारा फैलाई गई इस बात का भी जवाब देते हुए कि इस्लाम एक भय का धर्म है, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ईश्वर (अत्यंत दयालु, अत्यंत दयावान) है, तथा निन्यानवे नामों में से - सुन्दर ईश्वरीय नाम - जिन्हें मुसलमान दोहराते हैं, केवल दो नाम ऐसे हैं जो ईश्वरीय स्वरूप को शक्तिशाली, भयानक और दंड देने वाला बताते हैं, तथा इन दो विशेषताओं का प्रयोग केवल पापियों और अविश्वासियों के संदर्भ में ही किया जाता है।
यहाँ हम इस्लाम धर्म अपनाने के बाद लुई जार्डेट के जीवन में आए परिवर्तन की व्यापकता को देखते हैं। यह व्यक्ति अब पूरी ताकत से इस्लाम का बचाव कर रहा है, जबकि हाल ही में वह गैर-मुस्लिम बना था। ईश्वर की महिमा हो, जिसने उसे इस्लाम की ओर मार्गदर्शित किया!
स्रोत: डॉ. राघेब अल-सरजानी द्वारा लिखित पुस्तक (महान लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया)।
मोहम्मद फौद अल-हाशमी
उनका जन्म मिस्र में ईसाई माता-पिता के यहाँ हुआ था, जिन्होंने उनमें ईसाई धर्म के प्रति प्रेम का संचार किया ताकि वे अन्य ईसाइयों के साथ घुल-मिल सकें। हालाँकि, उन्होंने चिंतन और चर्चा शुरू की, और कुछ शंकाएँ उत्पन्न हुईं, जिसने उनके भीतर चिंता की ज्वाला को प्रज्वलित किया, जिसने उन्हें सत्य और सच्चे धर्म की खोज के लिए प्रेरित किया।
जब उनका मन बड़ा हुआ, तो उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। इस बारे में वे कहते हैं:
"अध्ययन के दौरान मुझे कई पुकारें ध्यान से सुनने को मिलीं, जो मेरे कानों तक पहुँचीं। ये पुकारें उन शंकाओं और संशय के अंतरालों के कारण आईं जो मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और भावनात्मक शुद्धता के क्षण में मेरी अंतरात्मा को आश्वस्त नहीं कर पा रही थी, जो मैं अध्ययन कर रहा था या कार्यों के संदर्भ में करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए उन पुकारों में सुनने का अंश था, जिसके बाद मेरे धर्म से पहले के धर्मों के बारे में चिंतन हुआ, इसलिए मैं मानो तवे से आग में शरण लेने वाले व्यक्ति की तरह था।"
मुहम्मद फुआद अल-हाशमी के इस्लाम धर्म अपनाने की कहानी
अल-हाशमी ने ईसाई-पूर्व धर्मों और मानव-निर्मित धर्मों पर शोध करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि उन्हें वह मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर उन्होंने इस्लाम पर शोध करना शुरू किया, लेकिन उन्हें इस्लाम से चिढ़ थी और वे उससे नफ़रत करते थे। वे इसमें प्रवेश नहीं करना चाहते थे; बल्कि, वे इसकी खामियों को उजागर करना चाहते थे, इसकी त्रुटियों को खोजना चाहते थे, और विरोधाभासों की खोज करना चाहते थे ताकि इसे ध्वस्त कर सकें और लोगों को इससे छुटकारा दिला सकें। लेकिन परिस्थितियों को बदलने वाले की जय हो! इस व्यक्ति को इस्लाम में मार्गदर्शन और प्रकाश का वह मार्ग मिला जिसकी तलाश वह जीवन भर करता रहा था।
इस्लामी धर्म में उन्होंने जो देखा, उसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं: "मुझे हर प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला, जो किसी भी पूर्ववर्ती धर्म को नहीं मिल सका, चाहे वह मानव निर्मित हो, ईश्वरीय धर्मों से उत्पन्न हो, या कोई दार्शनिक सिद्धांत हो (और मेरा यह कहना कि 'पतन' उन धर्मों के पतन को संदर्भित करता है जो उन पादरियों के हाथों हुए जो अपने उद्देश्य से भटक गए थे)। मैंने पाया कि वे जिन चीज़ों का दावा इस्लाम में कमियाँ मानते थे, वे गुण थे, और वे जिन्हें वे विरोधाभास मानते थे, वे ज्ञान, नियम और कानून थे जो समझदार लोगों के लिए बनाए गए थे। और जिस चीज़ के लिए वे इस्लाम की आलोचना करते थे, वह मानवता के लिए एक इलाज था, जो लंबे समय से अंधकार के जंगल में डूबी हुई थी, जब तक कि इस्लाम उसे अंधकार से प्रकाश में नहीं ले आया, और लोगों को उनके रब की अनुमति से सीधे मार्ग पर निर्देशित किया गया।"
इसके बाद मुहम्मद फुआद अल-हाशमी ने इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की।
मुहम्मद फुआद अल-हाशमी का योगदान
इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, मुहम्मद फुआद अल-हाशिमी ने इस्लाम की सेवा के लिए कई काम किए। उन्होंने धर्मों के बीच तुलनाएँ कीं, और इन तुलनाओं का एक परिणाम वह अद्भुत पुस्तक थी जो उन्होंने मुसलमानों को भेंट की, "रिलीजन्स इन द बैलेंस"। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें से सभी ने ईश्वर के वचन को मज़बूत करने और उनके धर्म का समर्थन करने का काम किया।
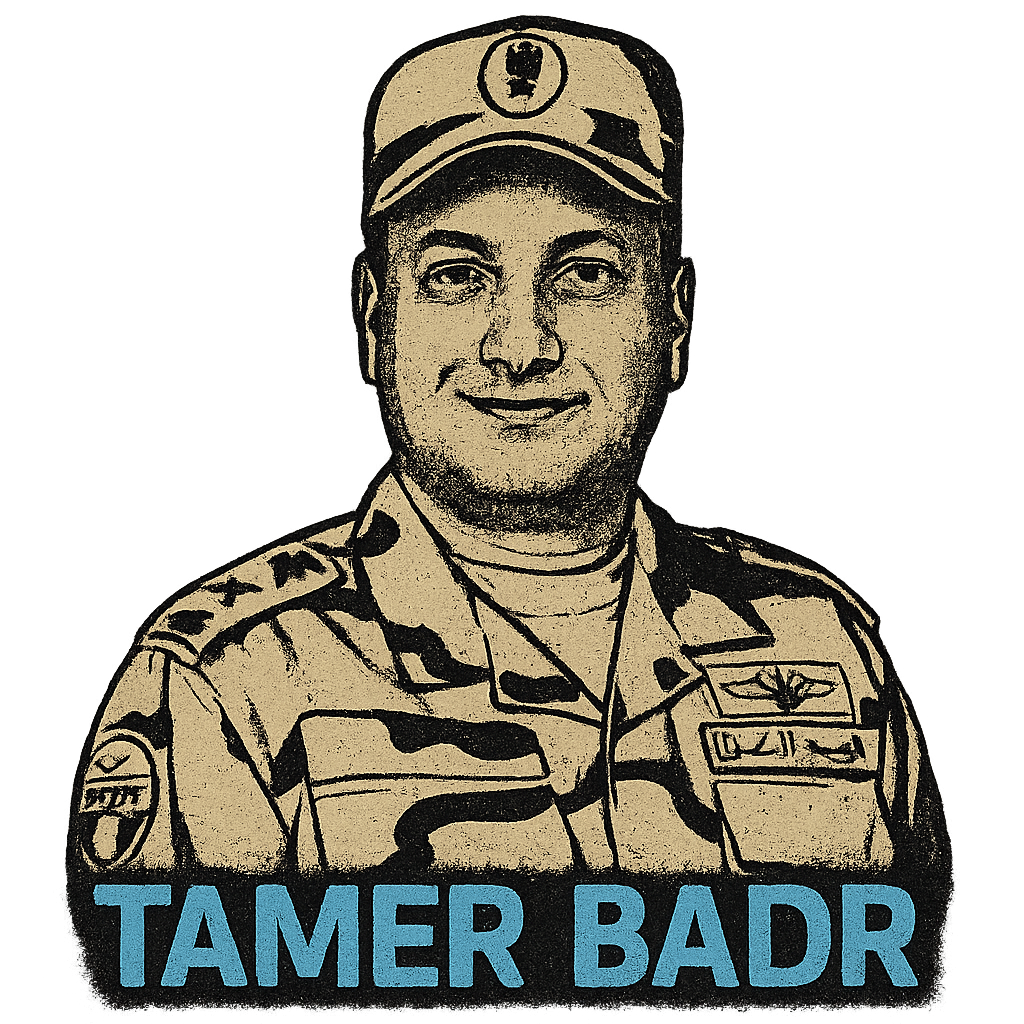
 अहमद नसीम सूसा, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर यहूदियों द्वारा लिखे गए झूठे इतिहास का सच उजागर किया, मूल रूप से यमन के हद्रामौत क्षेत्र में रहने वाली बानू सुवासा जनजाति के थे। उनका जन्म इराक के हिल्लाह शहर में 1318 हिजरी/1900 ई. में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 1924 ई. में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेरूत से अपनी प्रारंभिक शिक्षा (हाई स्कूल) पूरी की और फिर 1928 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
अहमद नसीम सूसा, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर यहूदियों द्वारा लिखे गए झूठे इतिहास का सच उजागर किया, मूल रूप से यमन के हद्रामौत क्षेत्र में रहने वाली बानू सुवासा जनजाति के थे। उनका जन्म इराक के हिल्लाह शहर में 1318 हिजरी/1900 ई. में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 1924 ई. में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेरूत से अपनी प्रारंभिक शिक्षा (हाई स्कूल) पूरी की और फिर 1928 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऐन सोफ़ी को यह एहसास नहीं था कि इस्लाम और मुसलमानों के मुद्दों में उनकी रुचि और उनका निष्पक्ष बचाव ही सच्चे धर्म को अपनाने की राह की शुरुआत थी। स्वीडन में जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया जाता, तो वह उन लोगों की राय का खंडन, बचाव और खंडन करने के लिए दौड़ पड़तीं जो उनका बुरा चाहते थे, अपने गंभीर विचारों और ठोस लेखों को प्रकाशित करके, जो प्रमाणों और तर्कों से समर्थित थे। इस प्रकार उन्होंने निष्पक्षता की दृष्टि से स्वीडिश समाज के साथ इस्लाम और मुसलमानों की सच्चाई पर खड़े होने की कोशिश की, कभी अखबारों में लेख लिखकर, कभी व्यापक रूप से वितरित विशिष्ट पुस्तकों के माध्यम से, और तीसरी बार प्रत्यक्ष बैठकों और सेमिनारों के माध्यम से।
ऐन सोफ़ी को यह एहसास नहीं था कि इस्लाम और मुसलमानों के मुद्दों में उनकी रुचि और उनका निष्पक्ष बचाव ही सच्चे धर्म को अपनाने की राह की शुरुआत थी। स्वीडन में जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया जाता, तो वह उन लोगों की राय का खंडन, बचाव और खंडन करने के लिए दौड़ पड़तीं जो उनका बुरा चाहते थे, अपने गंभीर विचारों और ठोस लेखों को प्रकाशित करके, जो प्रमाणों और तर्कों से समर्थित थे। इस प्रकार उन्होंने निष्पक्षता की दृष्टि से स्वीडिश समाज के साथ इस्लाम और मुसलमानों की सच्चाई पर खड़े होने की कोशिश की, कभी अखबारों में लेख लिखकर, कभी व्यापक रूप से वितरित विशिष्ट पुस्तकों के माध्यम से, और तीसरी बार प्रत्यक्ष बैठकों और सेमिनारों के माध्यम से। मार्टिन लिंग्स कौन हैं?
मार्टिन लिंग्स कौन हैं? एतान डाइन कौन है?
एतान डाइन कौन है? रेने गुएनोन कौन है?
रेने गुएनोन कौन है?